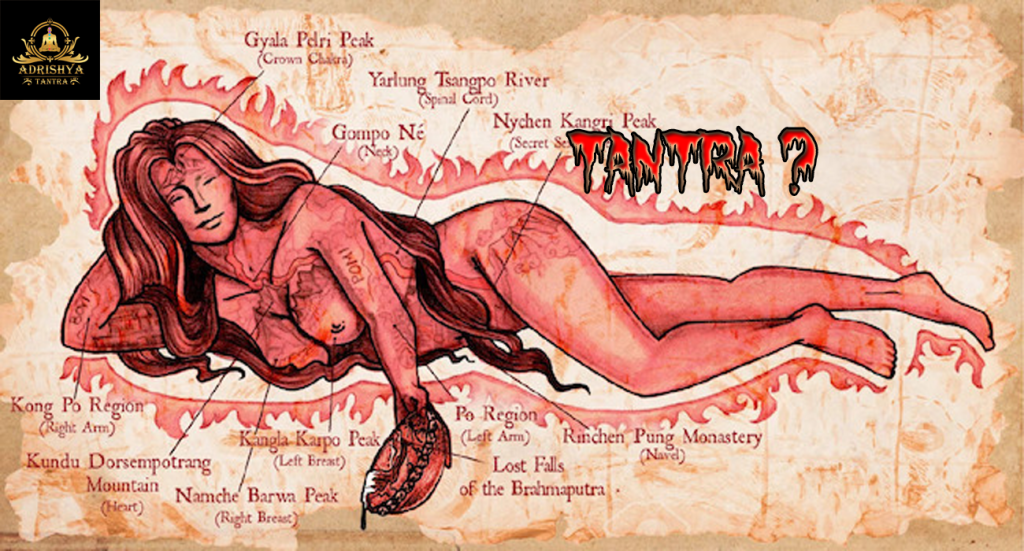तांत्रिक कला। ऊपरी बाएं से दक्षिणावर्त: वज्रयोगिनी (बौद्ध), श्री यंत्र (हिंदू), चक्र चित्रण, तिब्बत देवता वज्रधारा (वज्र धारक) मैथुना में , कालचक्र मंडला , ललिता त्रिपुरासुंदरी ।
सामान्य युग की प्रारंभिक शताब्दियों में, विष्णु , शिव या शक्ति पर केंद्रित नए प्रकट तंत्रों का उदय हुआ। [६] आधुनिक हिंदू धर्म के सभी मुख्य रूपों में तांत्रिक वंश हैं, जैसे शैव सिद्धांत परंपरा, श्री-विद्या का शाक्त संप्रदाय , कौला और कश्मीर शैववाद ।
बौद्ध धर्म में, वज्रयान परंपराओं को तांत्रिक विचारों और प्रथाओं के लिए जाना जाता है, जो भारतीय बौद्ध तंत्र पर आधारित हैं । [७] [८] इनमें भारत-तिब्बत बौद्ध धर्म , चीनी गूढ़ बौद्ध धर्म , जापानी शिंगोन बौद्ध धर्म और नेपाली नेवार बौद्ध धर्म शामिल हैं ।
तांत्रिक हिंदू और बौद्ध परंपराओं ने अन्य पूर्वी धार्मिक परंपराओं जैसे जैन धर्म , तिब्बती बॉन परंपरा, दाओवाद और जापानी शिंटो परंपरा को भी प्रभावित किया है । [९]
गैर- वैदिक पूजा के कुछ तरीके जैसे पूजा को उनके गर्भाधान और अनुष्ठानों में तांत्रिक माना जाता है। हिंदू मंदिर की इमारत भी आम तौर पर तंत्र की प्रतिमा के अनुरूप होती है। [१०] [११] इन विषयों का वर्णन करने वाले हिंदू ग्रंथों को तंत्र, आगम या संहिता कहा जाता है । [१२] [१३] बौद्ध धर्म में, तंत्र ने तिब्बती और पूर्वी एशियाई बौद्ध धर्म की कला और प्रतिमा के साथ-साथ भारत के ऐतिहासिक गुफा मंदिरों और दक्षिण पूर्व एशिया की कला को प्रभावित किया है । [१४] [१५] [१६]
शब्द-साधन
तंत्र ( संस्कृत : तन्त्र ) का शाब्दिक अर्थ है “करघा, ताना, बुनाई”। [१७] [२] [१८] पैडौक्स के अनुसार, मौखिक जड़ टैन का अर्थ है: “विस्तार करना”, “फैलना”, “बाहर निकालना”, “बुनाई”, “प्रदर्शन”, “आगे रखना”, और ” रचना”। इसलिए, विस्तार से, इसका अर्थ “प्रणाली”, “सिद्धांत” या “कार्य” भी हो सकता है। [19]
तंत्र शब्द का अर्थ एक गूढ़ अभ्यास या धार्मिक कर्मकांड है, जो एक औपनिवेशिक युग का यूरोपीय आविष्कार है। [20] [21] [22] इस अवधि के रूपक पर आधारित है बुनाई , रॉन बैरेट, कहा गया है जहां संस्कृत मूल तन साधन मुड़ने करघा पर धागे की। [२] इसका तात्पर्य एक पाठ, तकनीक या अभ्यास में “परंपराओं और शिक्षाओं को धागे के रूप में जोड़ना” है। [२] [१८]
यह शब्द ऋग्वेद के भजनों में प्रकट होता है जैसे कि 10.71 में, ” ताना (बुनाई) ” के अर्थ के साथ । [१७] [२३] यह कई अन्य वैदिक युग के ग्रंथों में पाया जाता है , जैसे कि अथर्ववेद की धारा १०.७.४२ और कई ब्राह्मणों में । [१७] [२४] इन और उत्तर-वैदिक ग्रंथों में, तंत्र का प्रासंगिक अर्थ वह है जो “मुख्य या आवश्यक भाग, मुख्य बिंदु, मॉडल, रूपरेखा, विशेषता” है। [१७] हिंदू धर्म (और जैन धर्म) के स्मृतियों और महाकाव्यों में, शब्द का अर्थ है “सिद्धांत, नियम, सिद्धांत, विधि, तकनीक या अध्याय” और यह शब्द एक अलग शब्द और एक सामान्य प्रत्यय के रूप में प्रकट होता है, जैसे कि आत्मा- तंत्र “सिद्धांत या सिद्धांत के अर्थ आत्मा (आत्मा, आत्म)”। [17] [24]
शब्द “तंत्र” लगभग 500 ईसा पूर्व के बाद, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म में एक ग्रंथ सूची श्रेणी है, जैसे सूत्र शब्द (जिसका अर्थ है “एक साथ सिलाई करना”, तंत्र में “एक साथ बुनाई” के रूपक को प्रतिबिंबित करना )। वही बौद्ध ग्रंथों को कभी-कभी तंत्र या सूत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है; उदाहरण के लिए, वैरोकाभिसंबोधि-तंत्र को वैरोकाभिसंबोधि-सूत्र भी कहा जाता है । [२५] तंत्र शब्द के विभिन्न प्रासंगिक अर्थ भारतीय पाठ के साथ बदलते हैं और उन्हें संलग्न तालिका में संक्षेपित किया गया है।
भारतीय ग्रंथों में “तंत्र” शब्द का प्रकट होना
परिभाषा
प्राचीन और मध्यकालीन युग
5 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान पाणिनी ने संस्कृत व्याकरण के अपने सूत्र 1.4.54-55 में, तंत्र को “स्व-तंत्र” (संस्कृत: स्वतन्त्र) के उदाहरण के माध्यम से गुप्त रूप से समझाया, जिसका अर्थ है “स्वतंत्र” या एक व्यक्ति जो उसका है खुद का “ताना, कपड़ा, बुनकर, प्रमोटर, कर्ता (अभिनेता)”। [27] पतंजलि अपने में महाभाष्य उद्धरण और पाणिनी की परिभाषा है, तो चर्चा स्वीकार करता है या एक अधिक से अधिक लंबाई में यह उल्लेख है, 18 मामलों में, उन्होंने कहा कि “ताना (बुनाई), विस्तारित कपड़ा” की अपनी प्रतीकात्मक परिभाषा कई संदर्भों के लिए प्रासंगिक है। [४०] तंत्र शब्द , पतंजलि कहता है, जिसका अर्थ है “प्रमुख, मुख्य”।
वह “स्व” (स्व) और तंत्र के एक संयुक्त शब्द के रूप में स्वतंत्र के समान उदाहरण का उपयोग करता है , फिर “स्वतंत्र” का अर्थ है “जो आत्म-निर्भर है, जो स्वयं का स्वामी है, जिसके लिए मुख्य चीज स्वयं है” , जिससे तंत्र की परिभाषा की व्याख्या होती है। [२७] पतंजलि तंत्र की एक अर्थपूर्ण परिभाषा भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि यह संरचनात्मक नियम, मानक प्रक्रियाएं, केंद्रीकृत मार्गदर्शिका या किसी भी क्षेत्र में ज्ञान है जो कई तत्वों पर लागू होता है। [40]
हिंदू धर्म का प्राचीन मीमांसा स्कूल तंत्र शब्द का व्यापक रूप से उपयोग करता है, और इसके विद्वान विभिन्न परिभाषाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए:
जब कोई कार्य या वस्तु, एक बार पूर्ण हो जाने पर, एक व्यक्ति या कई लोगों के लिए कई मामलों में फायदेमंद हो जाती है, जिसे तंत्र के रूप में जाना जाता है । उदाहरण के लिए, कई पुजारियों के बीच रखा गया दीपक। इसके विपरीत, जो इसके दोहराव से लाभान्वित होता है , उसे अश्वप कहा जाता है , जैसे कि तेल से मालिश करना। (…)
- सबारा, छठी शताब्दी, [२९] [४१]
मध्यकालीन ग्रंथ तंत्र की अपनी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। कामिका-तंत्र , उदाहरण के लिए, तंत्र शब्द की निम्नलिखित व्याख्या देता है :
क्योंकि यह ( तन ) प्रचुर और गहन मामलों को विस्तृत करता है, विशेष रूप से वास्तविकता ( तत्व ) और पवित्र मंत्रों के सिद्धांतों से संबंधित है , और क्योंकि यह मुक्ति ( त्र ) प्रदान करता है , इसे तंत्र कहा जाता है । [35]
आधुनिक युग
तांत्रिक और व्यवसायी पियरे बर्नार्ड (1875-1955) को व्यापक रूप से अमेरिकी लोगों के लिए तंत्र के दर्शन और प्रथाओं को पेश करने का श्रेय दिया जाता है, साथ ही साथ सेक्स के संबंध में एक भ्रामक धारणा पैदा करता है। [42]
आधुनिक विद्वता में, तंत्र का अध्ययन एक गूढ़ अभ्यास और कर्मकांडी धर्म के रूप में किया गया है, जिसे कभी-कभी तंत्रवाद कहा जाता है। तंत्र का अपने अनुयायियों के लिए क्या अर्थ है, और जिस तरह से तंत्र का प्रतिनिधित्व या माना जाता है, उसके बीच एक व्यापक अंतर है जब से औपनिवेशिक युग के लेखकों ने इस पर टिप्पणी करना शुरू किया। [४३] तब से तंत्र की कई परिभाषाएँ प्रस्तावित की गई हैं, और कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। [४४] आंद्रे पैडौक्स, तंत्र की परिभाषाओं की अपनी समीक्षा में दो प्रस्ताव देते हैं, फिर दोनों को अस्वीकार करते हैं। एक परिभाषा, पैडौक्स के कारण, तंत्र चिकित्सकों के बीच पाई जाती है – यह मनुष्य और ब्रह्मांड की दृष्टि के बारे में “अनुष्ठानों की प्रणाली” है जहां व्यक्ति की आंतरिक दुनिया और मैक्रोकॉस्मिक वास्तविकता के बीच पत्राचार एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। एक और परिभाषा, जो पर्यवेक्षकों और गैर-चिकित्सकों के बीच अधिक आम है, कुछ “यांत्रिक अनुष्ठानों का सेट, पूरी तरह से वैचारिक पक्ष को छोड़कर” है। [45]
तांत्रिक परम्पराओं का अध्ययन ज्यादातर पाठ्य और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया है। जीवित तांत्रिक परंपरा पर मानवशास्त्रीय कार्य दुर्लभ है, और नृवंशविज्ञान शायद ही कभी तंत्र के अध्ययन से जुड़ा हो। यह यकीनन तंत्र-मंत्र के तंत्र-मंत्र के आधुनिक निर्माण का परिणाम है, जो गुप्त, गूढ़ और गुप्त है। कुछ विद्वानों ने जीवित तांत्रिक परंपराओं के अध्ययन में नैतिक और ज्ञान – मीमांसा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए नए तरीके सुझाते हुए समकालीन तांत्रिक परंपराओं में रहस्य के मिथक को तोड़ने की कोशिश की है । [46]
डेविड एन. लोरेंजेन के अनुसार, तंत्र की दो अलग-अलग प्रकार की परिभाषाएं मौजूद हैं, संकीर्ण और व्यापक। [१३] संकीर्ण परिभाषा के अनुसार, तंत्रवाद, या “तांत्रिक धर्म”, तंत्र, संहिता और आगम नामक संस्कृत ग्रंथों पर सीधे आधारित कुलीन परंपराएं हैं। [१३] [४७] लोरेंजेन की “व्यापक परिभाषा” योग और शक्तिवाद जैसे “जादुई विश्वासों और प्रथाओं” की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करके इसका विस्तार करती है । [४७] [४८]
रिचर्ड पायने का कहना है कि लोकप्रिय संस्कृति के अंतरंगता के प्रति जुनून को देखते हुए तंत्र आमतौर पर सेक्स से गलत तरीके से जुड़ा हुआ है। तंत्र को “परमानंद के योग” के रूप में लेबल किया गया है, जो संवेदनहीन कर्मकांडवादी स्वतंत्रतावाद से प्रेरित है । [२५] यह उन बौद्धों, हिंदू और जैनियों के लिए तंत्र के अर्थ की विविध और जटिल समझ से बहुत दूर है जो इसका अभ्यास करते हैं। [25]
डेविड ग्रे व्यापक सामान्यीकरण से असहमत हैं और कहते हैं कि तंत्र को परिभाषित करना एक कठिन काम है क्योंकि “तंत्र परंपराएं कई गुना हैं, कई धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक दुनिया में फैली हुई हैं। परिणामस्वरूप वे विविध भी हैं, जो इसे पर्याप्त रूप से आने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनाती है। परिभाषा”। [४९] तंत्र को परिभाषित करने की चुनौती इस तथ्य से बढ़ जाती है कि यह दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के भीतर और बाहर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म सहित प्रमुख भारतीय धर्मों का ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। [५०] अपने अभ्यासकर्ताओं के लिए, तंत्र को ग्रंथों, तकनीकों, अनुष्ठानों, मठ प्रथाओं, ध्यान, योग और विचारधारा के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है। [51]
जॉर्ज फ्यूएरस्टीन के अनुसार , “तंत्रों में चर्चा किए गए विषयों का दायरा काफी है। वे दुनिया के निर्माण और इतिहास से संबंधित हैं; विभिन्न प्रकार के नर और मादा देवताओं और अन्य उच्च प्राणियों के नाम और कार्य; अनुष्ठान के प्रकार पूजा (विशेष रूप से देवी की); जादू, टोना, और अटकल; गूढ़ “फिजियोलॉजी” (सूक्ष्म या मानसिक शरीर का मानचित्रण); रहस्यमय सर्प शक्ति का जागरण (कुंडलिनी-शक्ति); शारीरिक और मानसिक शुद्धि की तकनीक; आत्मज्ञान की प्रकृति; और कम से कम, पवित्र कामुकता नहीं।” [५२] हिंदू पूजा , मंदिर और प्रतिमा सभी तांत्रिक प्रभाव दिखाते हैं। [१०] इन ग्रंथों में, गेविन फ्लड कहते हैं, “दर्शन में शरीर, अनुष्ठान और कला में” का प्रतिनिधित्व होता है, जो “शरीर की तकनीकों, विधियों या तकनीकों से जुड़े होते हैं जो शरीर और स्वयं को बदलने के उद्देश्य से तांत्रिक परंपराओं के भीतर विकसित होते हैं। “. [53]
तंत्र
तंत्रवाद शब्द 19वीं सदी का यूरोपीय आविष्कार है जो किसी एशियाई भाषा में मौजूद नहीं है; [२१] समान प्राच्यवादी मूल के ” सूफीवाद ” की तुलना करें । Padoux के अनुसार, तंत्र एक है पश्चिमी अवधि और धारणा, नहीं एक वर्ग है कि “Tantrists” खुद से प्रयोग किया जाता है। [२०] [नोट ४] यह शब्द १९वीं सदी के भारतविदों द्वारा पेश किया गया था, जिन्हें भारत का सीमित ज्ञान था और जिनके विचार में तंत्रवाद भारतीय परंपराओं के विपरीत एक विशेष, असामान्य और अल्पसंख्यक प्रथा थी जिसे वे मुख्यधारा मानते थे। [20]

तंत्र विद्या के तत्व। ऊपरी बाएँ से दक्षिणावर्त: मंत्र (बौद्ध), मंडला (हिंदू), यंत्र (काली का), खोपड़ी का प्याला (कपाल), नाड़ियाँ और चक्र (तिब्बती), यौन संघ में दर्शाए गए देवता। तंत्रवाद में ये न तो अनिवार्य हैं और न ही सार्वभौमिक। [54]
रॉबर्ट ब्राउन इसी तरह नोट करते हैं कि “तंत्रवाद” पश्चिमी विद्वता का निर्माण है , न कि धार्मिक व्यवस्था की अवधारणा। [५५] उन्होंने तंत्रवाद को एक ऐसी प्रणाली के लिए पश्चिमी लोगों के क्षमाप्रार्थी लेबल के रूप में परिभाषित किया है जिसे वे कम समझते हैं जो “सुसंगत नहीं है” और जो “विभिन्न स्रोतों से प्रथाओं और विचारों का एक संचित समूह है, जो एक समूह के भीतर अपने चिकित्सकों के बीच भिन्न है, सभी समूहों में, भूगोल में और इसके इतिहास में भिन्न है”। यह एक प्रणाली है, ब्राउन कहते हैं, जो प्रत्येक अनुयायी को तांत्रिक तत्वों को गैर-तांत्रिक पहलुओं के साथ मिलाने की स्वतंत्रता देता है, किसी भी और सभी मानदंडों को चुनौती देने और उल्लंघन करने के लिए, “सुपरमुंडन तक पहुंचने के लिए सांसारिक” के साथ प्रयोग करें। [44]
ट्यून गौड्रियान ने 1981 में हिंदू तंत्रवाद की अपनी समीक्षा में कहा है कि तंत्रवाद का अर्थ आमतौर पर “मोक्ष या आध्यात्मिक उत्कृष्टता के लिए व्यवस्थित खोज” है, जो कि अपने शरीर के भीतर परमात्मा को महसूस करने और बढ़ावा देने के लिए है, जो कि मर्दाना-स्त्री और आत्मा-पदार्थ का एक साथ मिलन है। , और “अद्वैत की प्रारंभिक आनंदमय अवस्था” को साकार करने का अंतिम लक्ष्य है। [५६] यह आम तौर पर एक व्यवस्थित रूप से प्रयास की गई प्रणाली है, जिसमें स्वेच्छा से चुनी गई विशिष्ट प्रथाएं शामिल हैं, जिसमें मंत्र ( बिजस ), ज्यामितीय पैटर्न और प्रतीक ( मंडल ), हावभाव ( मुद्रा ), किसी के शरीर के भीतर सूक्ष्म जगत का मानचित्रण जैसे तांत्रिक आइटम शामिल हो सकते हैं। सूक्ष्म शरीर ( कुंडलिनी योग ), प्रतीकों और ध्वनियों ( न्यासा ), ध्यान ( ध्यान ), अनुष्ठान पूजा ( पूजा ), दीक्षा ( दीक्षा ) और अन्य के रूप में बाहर के स्थूल तत्व । [५७] तंत्रवाद, गौड्रियान कहते हैं, एक जीवित प्रणाली है जो निश्चित रूप से अद्वैतवादी है , लेकिन व्यापक विविधताओं के साथ है, और एक सरल या निश्चित परिभाषा के बारे में हठधर्मिता होना असंभव है। [58]
तंत्रवाद “तांत्रिक परंपराओं” के लिए एक व्यापक शब्द है, डेविड ग्रे ने 2016 की समीक्षा में कहा है, जो प्राचीन हिंदू धर्म के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी बौद्ध और जैन परंपराओं से वैदिक, योगिक और ध्यान परंपराओं को जोड़ती है। [४३] यह पश्चिमी विद्वानों का एक नवशास्त्र है और किसी विशेष तांत्रिक परंपरा की आत्म-समझ को नहीं दर्शाता है। जबकि गौड्रियान का विवरण उपयोगी है, ग्रे कहते हैं, एक खुली विकसित प्रणाली होने के नाते, सभी तंत्र परंपराओं के लिए कोई एकल परिभाषित सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। [२२] तंत्रवाद, चाहे वह बौद्ध हो या हिंदू, को प्रथाओं के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है, तकनीकों का एक सेट, अनुष्ठानों और ध्यान पर एक मजबूत ध्यान के साथ, जो मानते हैं कि यह मुक्ति का मार्ग है जो ज्ञान और स्वतंत्रता दोनों की विशेषता है। . [59]
तांत्रिक:
पैडौक्स के अनुसार, “तांत्रिका” शब्द मानव धर्मशास्त्र २.१ पर कुल्लुका भट्ट की एक टिप्पणी पर आधारित है , जिन्होंने श्रुति (विहित ग्रंथों) के वैदिक और तांत्रिक रूपों के विपरीत किया । भट्ट के लिए तांत्रिक वह साहित्य है जो वैदिक संग्रह से स्वतंत्र हिंदू परंपरा का एक समानांतर हिस्सा है। वैदिक और गैर-वैदिक (तांत्रिक) पथों को परम वास्तविकता के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के रूप में देखा जाता है , वैदिक दृष्टिकोण ब्राह्मण पर आधारित है , और तांत्रिका गैर-वैदिक अगम ग्रंथों पर आधारित है । [६०] भट्ट ने स्पष्ट करने के प्रयास के बावजूद, पैडौक्स कहते हैं, वास्तव में हिंदुओं और बौद्धों ने ऐतिहासिक रूप से सभी स्रोतों, वैदिक, गैर-वैदिक और बौद्ध धर्म के मामले में, अपने स्वयं के विहित कार्यों से विचारों को उधार लेने और मिश्रण करने के लिए स्वतंत्र महसूस किया है। [61]
तांत्रिक और गैर-तांत्रिक परंपराओं के बीच महत्वपूर्ण अंतरों में से एक – चाहे वह रूढ़िवादी बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म हो – मठवासी या तपस्वी जीवन की आवश्यकता के बारे में उनकी धारणा है। [६२] सभी तीन प्रमुख प्राचीन भारतीय धर्मों में गैर-तांत्रिक, या रूढ़िवादी परंपराओं का मानना है कि एक गृहस्थ का सांसारिक जीवन इच्छाओं और लालचों से प्रेरित होता है जो आध्यात्मिक मुक्ति (मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य ) के लिए एक गंभीर बाधा है । ये रूढ़िवादी परंपराएं गृहस्थ जीवन का त्याग, एक भिक्षुक का सादगीपूर्ण जीवन और सभी मोहों को छोड़कर साधु या नन बनना सिखाती हैं। इसके विपरीत, तांत्रिक परंपराएं पकड़ती हैं, रॉबर्ट ब्राउन कहते हैं, कि “ज्ञान और सांसारिक सफलता दोनों” प्राप्त करने योग्य हैं, और “इस दुनिया को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए त्यागने की आवश्यकता नहीं है”। [62] [63]
इतिहास
वैदिक धर्म में आद्य-तांत्रिक तत्व
ऋग्वेद (१०.१३६) का केसिन भजन “जंगली कुंवारा” का वर्णन करता है, जो कारेल वर्नर कहते हैं, “अपने भीतर आग और जहर, स्वर्ग और पृथ्वी को लेकर, उत्साह और रचनात्मकता से लेकर अवसाद और पीड़ा तक, आध्यात्मिक आनंद की ऊंचाइयों से पृथ्वी से बंधे श्रम के भारीपन के लिए”। [६४] ऋग्वेद इन कुंवारे लोगों के लिए प्रशंसा के शब्दों का उपयोग करता है, [६४] और यह तंत्र से संबंधित है या नहीं, इसकी विभिन्न व्याख्या की गई है। डेविड लोरेंज़ेन के अनुसार, यह वर्णन करता है मुनियों (संतों) का सामना तंत्र की तरह “उन्मादपूर्ण, चेतना की बदल राज्यों” और क्षमता “हवा पर उड़ान भरने के लिए” प्राप्त कर रहा। [६५] इसके विपरीत, वर्नर का सुझाव है कि ये प्राचीन पूर्व-बौद्ध भारतीय परंपरा के प्रारंभिक योग अग्रदूत और निपुण योगी हैं, और यह वैदिक भजन उन “विचारों में खोए हुए” की बात कर रहा है जिनके “व्यक्तित्व पृथ्वी से बंधे नहीं हैं, क्योंकि वे रहस्यमय हवा के मार्ग का अनुसरण करते हैं”। [64]
दो सबसे पुराने उपनिषदों हिंदू धर्म, के शास्त्रों बृहदअरण्यक उपनिषद खंड 4.2 और में चंडोज्ञ उपनिषद खंड 8.6 में, का उल्लेख नाड़ियों ( hati कैसे पर अपने सिद्धांत पेश करने में) आत्मा ऊर्जा के माध्यम से (आत्मा) और शरीर से जुड़े हुए हैं और अन्योन्याश्रित ले जाने धमनियों जब कोई जाग रहा है या सो रहा है, लेकिन वे तांत्रिक साधनाओं से संबंधित किसी भी बात का उल्लेख नहीं करते हैं। [66] श्वेताश्वतारा उपनिषद का वर्णन करता है श्वास नियंत्रण है कि योग का एक मानक हिस्सा बन गया, लेकिन तांत्रिक प्रथाओं उस में नहीं दिखाई देते। [६५] [६७] इसी तरह, तैत्तिरीय उपनिषद शरीर के माध्यम से चलने वाले एक केंद्रीय चैनल की चर्चा करता है और विभिन्न वैदिक ग्रंथों में शारीरिक प्राण (महत्वपूर्ण श्वास) का उल्लेख है जो शरीर में घूमते हैं और इसे चेतन करते हैं। हालाँकि, योग के माध्यम से शरीर के प्राणों को सचेत रूप से स्थानांतरित करने का विचार इन स्रोतों में नहीं मिलता है। [68] Lorenzen के अनुसार, शरीर से संबंधित वैदिक विचारों बाद में क्षेत्र में अपना विस्तार “रहस्यमय रचना” की नाड़ियों और चक्रों तंत्र में पाया। [69] तंत्र के योग घटक में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है बाणभट्ट के हर्षचरित और दण्डी के दशकुमारचरित । [७०] लोरेंजेन के इस सिद्धांत के विपरीत, मिर्सिया एलियाडे जैसे अन्य विद्वान योग और योगिक प्रथाओं के विकास को तंत्र और तांत्रिक प्रथाओं के विकास से अलग और अलग मानते हैं। [71]
जेफ्री सैमुअल के अनुसार , तपस नामक आध्यात्मिक ऊर्जा का आंतरिक विकास ब्राह्मणों और श्रौत ग्रंथों में वैदिक धर्म का एक केंद्रीय तत्व बन जाता है । इन ग्रंथों में, तपस्वी प्रथाएं एक पवित्र व्यक्ति को तपस बनाने की अनुमति देती हैं, एक प्रकार की जादुई आंतरिक गर्मी, जो उन्हें सभी प्रकार के जादुई करतब करने के साथ-साथ दर्शन और दिव्य रहस्योद्घाटन करने की अनुमति देती है। [७२] सैमुअल ने यह भी नोट किया कि महाभारत में , “योग” शब्द के सबसे सामान्य उपयोग में से एक का अर्थ है “एक मरते हुए योद्धा को योग के माध्यम से सूर्य के क्षेत्र में मृत्यु के समय स्थानांतरित करना, एक अभ्यास जो उपनिषदिक संदर्भों के साथ जुड़ता है चैनल सिर के मुकुट के मार्ग के रूप में जिसके द्वारा कोई सौर मंडल के माध्यम से ब्रह्म की दुनिया की यात्रा कर सकता है।” मृत्यु के समय अपनी चेतना को स्थानांतरित करने की यह प्रथा अभी भी तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रथा है। [७३] सैमुअल ने यह भी नोट किया कि उपनिषदों में यौन अनुष्ठानों और आध्यात्मिक कामुकता का उल्लेख किया गया है। सैमुअल के अनुसार, “देर से वैदिक ग्रंथों में संभोग को प्रतीकात्मक रूप से वैदिक बलिदान के बराबर माना जाता है , और वीर्य के स्खलन को प्रसाद के रूप में माना जाता है।” इस विषय में पाया जा सकता Jaiminiya ब्राह्मण , चंडोज्ञ उपनिषद , और Brhadaranyaka उपनिषद । Brhadaranyaka विभिन्न यौन रस्में और प्रथाओं जो ज्यादातर एक बच्चे जो पुरुष पौरूष और बिजली की हानि को लेकर चिंतित हैं प्राप्त करने के उद्देश्य होते हैं। [74]
डेविड गॉर्डन व्हाइट विचार योगिनी विद्वानों ने का कहना है कि इस तरह के कई संप्रदायों की जड़ों में इस तरह स्वदेशी जनजातियों या के रूप में एक “मूल निवासी गैर वैदिक स्रोत” में झूठ के साथ जल्दी तंत्र लेकिन असहमत करने के लिए मूलभूत के रूप में कई संप्रदायों सिंधु घाटी सभ्यता । [75] इसके बजाय, व्हाइट पता चलता है वैदिक Srauta ग्रंथों एक तरह से एक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए इसी तरह के देवी-राका, Sinīvālī, और Kuhu को प्रसाद का उल्लेख है। [७६] फ्रेडरिक स्मिथ – संस्कृत और शास्त्रीय भारतीय धर्मों के एक प्रोफेसर, तंत्र को पहली सहस्राब्दी ईस्वी के भक्ति आंदोलन के समानांतर एक धार्मिक आंदोलन मानते हैं । [७७] तंत्र के साथ आयुर्वेद , स्मिथ कहते हैं, पारंपरिक रूप से अथर्ववेद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है , लेकिन यह विशेषता ऐतिहासिकता की नहीं सम्मान में से एक है। आयुर्वेद मुख्य रूप से वैदिक जड़ों के साथ एक अनुभवजन्य अभ्यास रहा है, लेकिन तंत्र बिना किसी आधार के एक गूढ़, लोक आंदोलन रहा है जिसे अथर्ववेद या किसी अन्य वैदिक पाठ में किसी भी चीज़ का पता लगाया जा सकता है । [77]
बौद्ध धर्म में आद्य-तांत्रिक तत्व
चीनी लिप्यंतरण के साथ सिद्धम लिपि में एक बौद्ध धारा ( भज ), नीलाहनामहृदय धारा ।
एक यक्षिक (द्वितीय शताब्दी), मथुरा क्षेत्र की कुषाण मूर्ति ।
पूर्व-तांत्रिक बौद्ध धर्म में ऐसे तत्व शामिल हैं जिन्हें प्रोटो-तांत्रिक के रूप में देखा जा सकता है, और जिन्होंने बौद्ध तांत्रिक परंपरा के विकास को प्रभावित किया हो सकता है। जादुई मंत्रों या मंत्रों का उपयोग प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों के साथ-साथ कुछ महायान सूत्रों में भी पाया जा सकता है। [७८] इन जादुई मंत्रों या मंत्रों का उपयोग विभिन्न कारणों से किया जाता था, जैसे कि सुरक्षा के लिए , और शुभता की उत्पत्ति के लिए । [७ ९ ] पाली परंपरा में, सुरक्षा मंत्रों को परिट्टा कहा जाता है , और इसमें रतन सुत्त जैसे ग्रंथ शामिल हैं जो आज थेरवाद परंपरा में व्यापक रूप से पढ़े जाते हैं । [८०] [८१] महायान मंत्रों को धारा कहा जाता है । कुछ महायान सूत्रों में मंत्रों का उपयोग शामिल है , जो तांत्रिक अभ्यास की एक केंद्रीय विशेषता है।
जेफ्री सैमुअल के अनुसार, बौद्ध और जैन जैसे श्रमण समूह मृतकों से जुड़े थे। सैमुअल ने नोट किया कि वे “अक्सर मृतकों से जुड़े स्थलों पर बस गए और ऐसा लगता है कि मृतकों की आत्माओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।” इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए भारतीय दृष्टिकोण से एक खतरनाक और अशुद्ध अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करना आवश्यक है। मृत्यु के साथ यह जुड़ाव आधुनिक बौद्ध धर्म की एक विशेषता बनी हुई है, और आज बौद्ध देशों में, बौद्ध भिक्षु और अन्य अनुष्ठान विशेषज्ञ मृतकों के प्रभारी हैं। [८२] इस प्रकार, तांत्रिक साधकों का धर्मस्थल और मृत्यु चित्रों के साथ जुड़ाव , मृतकों के इन स्थलों के साथ प्रारंभिक बौद्ध संपर्क से पहले है।
कुछ विद्वानों का मानना है कि तंत्र का विकास यक्षों और नागों जैसे प्रकृति आत्मा-देवताओं के पंथों से प्रभावित हो सकता है । [८३] यक्ष पंथ प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे । यक्ष शक्तिशाली प्रकृति की आत्माएं हैं जिन्हें कभी-कभी संरक्षक या रक्षक के रूप में देखा जाता था। [८४] कुबेर जैसे यक्ष भी जादुई मंत्रों से जुड़े हैं। कहा जाता है कि कुबेर ने बौद्ध संघ को साननीय सुत्त में सुरक्षा मंत्र प्रदान किए थे । [85] ये भावना देवी-देवताओं को भी शामिल कई महिला देवताओं (yakṣiṇī) पाया जा सकता है कि जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों में दिखाया गया सांची और भरहुत । जल्दी बौद्ध ग्रंथों में भी देवी-देवताओं को बुलाया तरह भयंकर दानव की उल्लेख है raksasa , और rākṣasī खाने बच्चों की तरह Hariti । [८६] वे महायान ग्रंथों में भी मौजूद हैं, जैसे लोटस सूत्र के अध्याय २६ में जिसमें बुद्ध और राक्षसों के एक समूह के बीच एक संवाद शामिल है, जो सूत्र को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने की शपथ लेते हैं। ये आंकड़े कमल सूत्र के अनुयायियों की रक्षा के लिए जादुई धारियाँ भी सिखाते हैं । [87]
बौद्ध तांत्रिक साधना का एक प्रमुख तत्व ध्यान में देवताओं का दर्शन है। यह प्रथा वास्तव में पूर्व-तांत्रिक बौद्ध ग्रंथों में भी पाई जाती है। प्रत्युत्पन्न समाधि और तीन अमिताभ शुद्ध भूमि सूत्र जैसे महायान सूत्रों में । [८८] अन्य महायान सूत्र हैं जिनमें “प्रोटो-तांत्रिक” सामग्री शामिल है जैसे कि गंडव्यूह और दसभुमिका जो बाद के तांत्रिक ग्रंथों में मिली कल्पना के स्रोत के रूप में काम कर सकती हैं। [८९] सैमुअल के अनुसार, गोल्डन लाइट सूत्र (सी। नवीनतम में ५वीं शताब्दी) में वह शामिल है जिसे प्रोटो-मंडल के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे अध्याय में, एक बोधिसत्व “बेरिल की और परमात्मा जवाहरात और खगोलीय इत्र के साथ किए गए एक विशाल इमारत का एक सपना है चार कमल-सीटें, चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं उन पर बैठा चार बुद्ध के साथ:। Aksobhya में पूर्व, Ratnaketu में दक्षिण, Amitayus पश्चिम और Dundubhīśvara उत्तर में है। ” [९०]
आधुनिक पाकिस्तान में गांधार में खोजी गई कलाकृति की एक श्रृंखला , लगभग पहली शताब्दी सीई से डेटिंग, बौद्ध और हिंदू भिक्षुओं को खोपड़ी पकड़े हुए दिखाती है। [९१] इन कलाकृतियों से संबंधित किंवदंती बौद्ध ग्रंथों में पाई जाती है, और भिक्षुओं का वर्णन करती है “जो खोपड़ी को टैप करते हैं और उस व्यक्ति के भविष्य के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी करते हैं जिससे वह खोपड़ी संबंधित थी”। [९१] [९२] रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार, इन बौद्ध खोपड़ी-टैपिंग राहतों से पता चलता है कि तांत्रिक प्रथाएं १ शताब्दी ईस्वी तक प्रचलन में रही होंगी। [91]
शक्तिवाद और शैववाद में आद्य-तांत्रिक तत्व
एक आधुनिक Aghori एक खोपड़ी कप (साथ Kapala )। उनके पूर्ववर्ती, मध्ययुगीन कपालिकाएं (“खोपड़ी-पुरुष”) आक्रामक या “बाएं हाथ” शैव तंत्र के विकास में प्रभावशाली व्यक्ति थे ।
महाभारत , हरिवंश पर्व , और देवी महात्म्य में मार्कंडेय पुराण सभी महान देवी, की भयंकर, दानव हत्या अभिव्यक्तियों का उल्लेख Mahishamardini , के साथ की पहचान दुर्गा – पार्वती । [९३] ये सुझाव देते हैं कि भारतीय संस्कृति में देवी के लिए शक्तिवाद , श्रद्धा और पूजा, पहली सहस्राब्दी की प्रारंभिक शताब्दियों तक एक स्थापित परंपरा थी। [९४] पैडौक्स ने ४२३-४२४ सीई के एक शिलालेख का उल्लेख किया है जिसमें भयानक देवताओं के लिए एक मंदिर की स्थापना का उल्लेख है जिसे “माँ” कहा जाता है। [९५] हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि तांत्रिक अनुष्ठान और प्रथाएं अभी तक हिंदू या बौद्ध परंपराओं का हिस्सा थीं। “423 सीई के गंगाधर शिलालेख में तंत्र के कुछ संदिग्ध संदर्भ के अलावा”, डेविड लोरेनजेन कहते हैं, यह केवल 7 वीं शताब्दी के बाणभट्ट की कादंबरी है जो तंत्र और तांत्रिक ग्रंथों का ठोस प्रमाण प्रदान करती है। [33]
ऐसा प्रतीत होता है कि शैव तपस्वी तंत्र के प्रारंभिक विकास में शामिल रहे हैं, विशेष रूप से धर्मग्रंथ से निपटने वाले अतिक्रमणकारी तत्व। सैमुअल के अनुसार, शैव तपस्वियों के एक समूह, पासुपतों ने आध्यात्मिकता के एक रूप का अभ्यास किया, जिसने बाद में एक तांत्रिक संदर्भ में पाए जाने वाले चौंकाने वाले और विवादित व्यवहार का उपयोग किया, जैसे नृत्य, गायन और खुद को राख से ढंकना। [96]
प्रारंभिक तांत्रिक प्रथाओं को कभी-कभी भैरव, कपालिका (“खोपड़ी पुरुष”, जिसे सोमसिद्धतिन या महावर्तिन भी कहा जाता है ) से जुड़े शैव तपस्वियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है । [९७] [९८] [९९] इस चौंकाने वाले तथ्य के अलावा कि वे श्मशान घाटों और मानव खोपड़ी ले जाते थे, उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, और कापालिकों पर प्राथमिक स्रोतों की कमी है। [१००] [९९] सैमुअल यह भी कहते हैं कि स्रोत उन्हें शराब और सेक्स का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के रूप में चित्रित करते हैं, कि वे योगिनिस और डाकिनिस नामक भयानक महिला आत्मा-देवताओं से जुड़े थे , और यह माना जाता था कि उनके पास उड़ान जैसी जादुई शक्तियां थीं। [101]
कापालिकों को काल्पनिक कार्यों में चित्रित किया गया है और पहली सहस्राब्दी सीई के बौद्ध, हिंदू और जैन ग्रंथों में भी व्यापक रूप से अपमानित किया गया है। [100] [102] में हाला की गाथा-saptasati (5 वीं शताब्दी ई द्वारा रचित), उदाहरण के लिए, कहानी एक महिला चरित्र कापालिक, जिसका प्रेमी मरता कहता है, वह अंतिम संस्कार किया जाता है, वह उनके अंतिम संस्कार राख लेता है और उसके शरीर स्मीयरों इसके साथ। [९८] ६वीं शताब्दी के वराहमिहिर ने अपने साहित्यिक कार्यों में कापालिकों का उल्लेख किया है। [१०२] इन ग्रंथों में वर्णित कुछ कापालिका प्रथाएं शैव हिंदू धर्म और वज्रयान बौद्ध धर्म में पाई जाती हैं, और विद्वान इस बात से असहमत हैं कि किसने किसको प्रभावित किया। [103] [104]
ये प्रारंभिक ऐतिहासिक उल्लेख पारित होने में हैं और तंत्र जैसी प्रथाओं के रूप में प्रतीत होते हैं, वे विस्तृत नहीं हैं और न ही तांत्रिक मान्यताओं और प्रथाओं की व्यापक प्रस्तुति हैं। कौल तांत्रिक प्रथाओं के पुरालेख संदर्भ दुर्लभ हैं। नौवीं शताब्दी की शुरुआत में कौल के वामा (बाएं हाथ) तंत्र का उल्लेख किया गया है। [१०५] साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि तांत्रिक बौद्ध धर्म संभवत: ७वीं शताब्दी तक फल-फूल रहा था। [६५] मातृका, या उग्र देवी जो बाद में तंत्र प्रथाओं से निकटता से जुड़ी हुई हैं, ७वीं और १०वीं शताब्दी के बीच बौद्ध और हिंदू कला और साहित्य दोनों में दिखाई देती हैं। [106]
तंत्र का उदय और विकास
भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में नृत्य भैरव
नृत्य वज्रवराही , एक बौद्ध तांत्रिक देवता, नेपाल , ११वीं-१२वीं शताब्दी।
एक योगी और उनके चक्रों का चित्रण ।

कर्ममुद्रा (“एक्शन सील”) के यौन योग का अभ्यास करने वाले बौद्ध महासिद्ध ।
गेविन फ्लड के अनुसार , तांत्रिक प्रथाओं से संबंधित तंत्र ग्रंथों की सबसे प्रारंभिक तिथि ६०० सीई है, हालांकि उनमें से अधिकांश की रचना संभवतः ८वीं शताब्दी के बाद की गई थी।
[१०७] बाढ़ के अनुसार, तंत्रों की रचना किसने की, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है और न ही इन और मध्यकालीन युग के तांत्रिकों की सामाजिक स्थिति के बारे में
ज्यादा जानकारी है।
फ्लड में कहा गया है कि तंत्र के अग्रदूत तपस्वी रहे होंगे जो श्मशान घाटों पर रहते थे, संभवतः “निम्न-जाति समूहों से ऊपर” से, और संभवतः गैर-ब्राह्मणवादी और संभवतः एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा थे। [१०९] [११०] [१११] प्रारंभिक मध्ययुगीन काल तक, उनकी प्रथाओं में मांसाहारी भोजन, शराब और यौन पदार्थों के प्रसाद के साथ काली और भैरव जैसे देवताओं की नकल शामिल हो सकती थी। इस सिद्धांत के अनुसार, इन चिकित्सकों ने अपने देवताओं को उनमें प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया होगा, फिर उस देवता को नियंत्रित करने और अपनी शक्ति हासिल करने के लिए भूमिका को वापस कर दिया। [१०८] इन तपस्वियों को श्मशान स्थलों पर रहने वाली निम्न जातियों का समर्थन प्राप्त होता। [१०८]
शमूएल कहा गया है कि नियम-कायदों से और antinomian दोनों बौद्ध और ब्राह्मण (मुख्य रूप से कापालिक तरह शैव संन्यासियों) संदर्भों और कहा कि “Śaivas और बौद्ध, एक दूसरे से बड़े पैमाने पर उधार ली गई पावती की डिग्री बदलती के साथ।” में विकसित तांत्रिक प्रथाओं सैमुअल के अनुसार, इन जानबूझकर उल्लंघनकारी प्रथाओं में शामिल हैं, “रात का समय चार्ल के मैदानों में होता है, जिसमें मानव मांस खाना, मानव हड्डियों से बने गहनों, कटोरे और संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग, लाशों पर बैठे यौन संबंध, और इसी तरह शामिल हैं। ” [११२]
शमूएल के अनुसार, तंत्र के विकास में एक अन्य प्रमुख तत्व था “स्थानीय और क्षेत्रीय देवता पंथों का क्रमिक परिवर्तन जिसके माध्यम से उग्र पुरुष और विशेष रूप से, महिला देवताओं ने यक्ष देवताओं के स्थान पर एक प्रमुख भूमिका निभाई।” सैमुअल का कहना है कि यह पांचवीं से आठवीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। [११३] सैमुअल के अनुसार, इन भयानक देवी-देवताओं पर दो मुख्य विद्वानों की राय है जो शिव और बौद्ध तंत्र में शामिल हो गए। पहला विचार यह है कि वे एक अखिल भारतीय धार्मिक आधार से उत्पन्न होते हैं जो वैदिक नहीं था। एक और मत है कि इन उग्र देवी-देवताओं को वैदिक धर्म से विकसित होते हुए देखना है। [११४]
एलेक्सिस सैंडरसन ने तर्क दिया है कि तांत्रिक प्रथाओं को मूल रूप से एक शैव परिवेश में विकसित किया गया था और बाद में बौद्धों द्वारा अपनाया गया था। उन्होंने शैव विद्यापीठ साहित्य में पाए जाने वाले कई तत्वों का हवाला दिया , जिसमें संपूर्ण मार्ग और पीठों की सूची शामिल है, जो कि वज्रयान ग्रंथों द्वारा सीधे उधार लिया गया लगता है। [११५] हालांकि, विद्यापीठ ग्रंथों की अनिश्चित तारीख के कारण रोनाल्ड एम. डेविडसन ने इसकी आलोचना की है । [११६] डेविडसन का तर्क है कि ऐसा लगता है कि पीठ न तो विशिष्ट रूप से बौद्ध थे और न ही शिव, लेकिन दोनों समूहों द्वारा अक्सर आते थे। उन्होंने यह भी कहा कि शैव परंपरा भी स्थानीय देवताओं के विनियोग में शामिल थी और यह तंत्र आदिवासी भारतीय धर्मों और उनके देवताओं से प्रभावित हो सकता है । [११७] सैमुअल लिखते हैं कि “नारी देवत्वों को एक विशिष्ट शाक्त परिवेश के संदर्भ में अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जिसमें से शैव और बौद्ध दोनों उधार ले रहे थे,” लेकिन यह कि अन्य तत्व, जैसे कि कपालिका शैली की प्रथाएं, अधिक स्पष्ट रूप से एक शैव से ली गई हैं। परंपरा। [118]
सैमुअल लिखते हैं कि शैव तंत्र परंपरा वंशानुगत जाति समूहों (कुलों) द्वारा किए गए अनुष्ठान टोना के रूप में उत्पन्न हुई है और सेक्स, मृत्यु और भयंकर देवी से जुड़ी हुई है। दीक्षा अनुष्ठान में एक पुरुष गुरु और उनकी पत्नी के मिश्रित यौन स्राव (कबीले का सार) का सेवन शामिल था। इन प्रथाओं को कपालिका शैली के तपस्वियों ने अपनाया और प्रारंभिक नाथ सिद्धों को प्रभावित किया। समय के साथ, अधिक चरम बाहरी तत्वों को आंतरिक योगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो सूक्ष्म शरीर का उपयोग करते हैं। यौन अनुष्ठान परंपरा में सिखाए गए मुक्ति ज्ञान तक पहुंचने का एक तरीका बन गया। [११९]
बौद्धों ने तंत्रों के अपने स्वयं के कोष का विकास किया, जो विभिन्न महायान सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ-साथ उग्र देवी परंपरा के तत्वों और शैव परंपराओं (जैसे भैरव जैसे देवताओं, जो कि होने के रूप में देखा गया था) के तत्वों पर भी आकर्षित हुए। अधीन और बौद्ध धर्म में परिवर्तित)। [१०७] [१२०] कुछ बौद्ध तंत्र (जिन्हें कभी-कभी “निचला” या “बाहरी” तंत्र कहा जाता है) जो पहले के कार्य हैं, वे अपराध, लिंग और उग्र देवताओं का उपयोग नहीं करते हैं। ये पहले के बौद्ध तंत्र मुख्य रूप से महायान सिद्धांत और व्यवहार (जैसे देवता दृश्य) के विकास और अनुष्ठान और शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। [१२१] आठवीं और दसवीं शताब्दी के बीच, नए तंत्रों का उदय हुआ जिनमें उग्र देवता, कुल शैली की यौन दीक्षा, सूक्ष्म शरीर अभ्यास और यौन योग शामिल थे। बाद के बौद्ध तंत्रों को “आंतरिक” या “अद्वितीय योग” ( अनुत्तरयोग या “योगिनी”) तंत्र के रूप में जाना जाता है । सैमुअल के अनुसार, ऐसा लगता है कि इन यौन प्रथाओं को शुरू में बौद्ध मठों द्वारा अभ्यास नहीं किया गया था और इसके बजाय यात्रा सिद्धों के बीच मठवासी प्रतिष्ठानों के बाहर विकसित किया गया था। [122]
तांत्रिक प्रथाओं में गुप्त दीक्षा समारोह भी शामिल थे जिसमें व्यक्ति तांत्रिक परिवार (कुल) में प्रवेश करते थे और तांत्रिक देवताओं के गुप्त मंत्र प्राप्त करते थे। इन दीक्षाओं में गुरु और उनकी पत्नी के बीच अनुष्ठानिक सेक्स के माध्यम से उत्पन्न यौन पदार्थों (वीर्य और महिला यौन स्राव) का सेवन शामिल था। इन पदार्थों को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता था और इन्हें तांत्रिक देवताओं के लिए प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। [१२३] शैवों और बौद्धों दोनों के लिए, तांत्रिक प्रथाएं अक्सर भयंकर देवी-देवताओं से जुड़े महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों (पीठों) पर होती थीं। [१२४] सैमुअल लिखते हैं कि “हमारे पास इस बात की स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि तीर्थ स्थलों का यह नेटवर्क कैसे पैदा हुआ।” जो भी हो, ऐसा लगता है कि बौद्धों और शैवों द्वारा देखे गए इन अनुष्ठान स्थलों में आठवीं और नौवीं शताब्दी के दौरान कौला और अनुत्तरयोग तंत्र का अभ्यास विकसित हुआ था। [१२५] ऊपर उल्लिखित प्रथाओं के अलावा, इन स्थलों में कामाख्या जैसी शाक्त देवियों को रक्तदान के रूप में पशु बलि की प्रथा भी देखी गई । इस अभ्यास का उल्लेख कालिकापुराण और योगिनीतंत्र जैसे शाक्त ग्रंथों में मिलता है । इनमें से कुछ स्थलों में, जैसे कामाख्या पीठ, शाक्तों द्वारा अभी भी पशु बलि का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। [१२६]
मध्ययुगीन तांत्रिक प्रणाली का एक अन्य प्रमुख और अभिनव सुविधा की सामग्री पर आधारित आंतरिक योग का विकास था सूक्ष्म शरीर ( sūkṣma śarīra )। इस सूक्ष्म शरीर रचना ने माना कि शरीर ( नाड़ियों ) में चैनल थे जिनके माध्यम से कुछ पदार्थ या ऊर्जा (जैसे वायु , प्राण , कुंडलिनी और शक्ति ) प्रवाहित होती थीं। इन योगों में इन ऊर्जाओं को शरीर के माध्यम से कुछ गांठों या रुकावटों ( ग्रंथी ) को दूर करने और ऊर्जा को केंद्रीय चैनल ( अवधूति, सुषुम्ना ) की ओर निर्देशित करना शामिल था। ये योगाभ्यास यौन योग के अभ्यास से भी निकटता से संबंधित हैं , क्योंकि संभोग को इन ऊर्जाओं के प्रवाह की उत्तेजना में शामिल होने के रूप में देखा गया था। [१२७] सैमुअल सोचता है कि सूक्ष्म शरीर की ये प्रथाएं चीनी दाओवादी प्रथाओं से प्रभावित हो सकती हैं । [128]
यौन योग अभ्यास के शुरुआती उल्लेखों में से एक असंग (सी। 5 वीं शताब्दी) के बौद्ध महायानसूत्रलंकार में है , जिसमें कहा गया है कि “सुखद बुद्ध-शिष्टता में संभोग के उलट और किसी की अदम्य दृष्टि में सर्वोच्च आत्म-नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। पति या पत्नी।” [१२९] डेविड स्नेलग्रोव के अनुसार , पाठ में ‘संभोग के उलट’ का उल्लेख स्खलन को रोकने की प्रथा का संकेत दे सकता है। स्नेलग्रोव का कहना है कि यह संभव है कि इस समय बौद्ध मंडलियों में पहले से ही यौन योग का अभ्यास किया जा रहा था, और असंग ने इसे एक वैध अभ्यास के रूप में देखा। [१३०] इसी तरह, सैमुअल सोचता है कि यौन योग चौथी या पांचवीं शताब्दी में मौजूद होने की संभावना है (हालांकि उसी आक्रामक तांत्रिक संदर्भों में नहीं जहां बाद में इसका अभ्यास किया गया था)। [१३१]
सातवीं और आठवीं शताब्दी में ही हमें इन यौन योगों के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। हालांकि, पिछले उपनिषद यौन अनुष्ठानों के विपरीत, जो वैदिक बलिदान और बच्चे के जन्म की तरह सांसारिक अंत से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, ये यौन योग सूक्ष्म शरीर ऊर्जा (जैसे कुंडलिनी और चांडाली , जिन्हें देवी के रूप में भी देखा जाता था) के आंदोलन से जुड़े थे , और यह भी आध्यात्मिक अंत के साथ। [१३२] ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रथाएं शैव और बौद्ध दोनों मंडलियों में लगभग एक ही समय में विकसित हुईं , और तिरुमुलर , गोरखनाथ , विरुपा , नरोपा जैसी आकृतियों से जुड़ी हैं । तांत्रिक महासिद्धों ने सूक्ष्म शरीर और यौन तत्वों के साथ योग प्रणाली विकसित की जिससे जादुई शक्तियां ( सिद्धियां ), अमरता , साथ ही आध्यात्मिक मुक्ति (मोक्ष, निर्वाण) हो सकती हैं। यौन योग को चेतना के आनंदमय विस्तार के उत्पादन के एक तरीके के रूप में देखा गया जो मुक्ति की ओर ले जा सकता है। [१३१]
जैकब डाल्टन के अनुसार, अनुष्ठानिक यौन योग (तांत्रिक दीक्षा अनुष्ठान के यौन तत्वों के साथ, जैसे यौन तरल पदार्थों का सेवन) सबसे पहले महायोग तंत्र (जिसमें गुह्यगर्भ और घुयसमाज शामिल हैं ) नामक बौद्ध कार्यों में दिखाई देता है । [१३३] [१३४] ये ग्रंथ “शरीर के आंतरिक भाग पर, पुरुष और महिला के यौन अंगों के शारीरिक विवरण और यौन मिलन के माध्यम से उत्पन्न आनंद पर केंद्रित हैं।” इन ग्रंथों में, यौन ऊर्जा को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में भी देखा गया था जिसे आध्यात्मिक अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और सैमुअल के अनुसार “शायद आनंद की स्थिति और व्यक्तिगत पहचान की हानि जो मुक्त अंतर्दृष्टि के साथ समरूप है।” [133] ये यौन योग अधिक जटिल प्रणालियों नौवें या दसवीं शताब्दी, शैव सहित के बारे में से डेटिंग ग्रंथों में पाए जाते हैं में आगे का विकास जारी रखा Kaulajñānanirṇaya और Kubjikātantra साथ ही बौद्ध के रूप में Hevajra , और Cakrasamvara तंत्र जो मेहराबदार छत से युक्त जमीन का इस्तेमाल करते हैं प्रतीकवाद और उग्र देवी। [१३५] सैमुअल लिखते हैं कि ये बाद के ग्रंथ भी यौन योग को सूक्ष्म शरीर की ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की प्रणाली के साथ जोड़ते हैं। [128]
तांत्रिक युग
बारह सशस्त्र Chakrasamvara और उनकी पत्नी Vajravarahi, सीए 12वीं सदी, भारत (बंगाल) या बांग्लादेश
योगिनी , पूर्वी भारत, 11वीं-12वीं शताब्दी ई. मात्सुओका कला संग्रहालय, टोक्यो, जापान Tokyo
हिरण्यवर्ण महाविहार में एक पत्थर कालाचक्र मंडल , नेपाल के पाटन में एक बौद्ध मंदिर , जिसे १२वीं शताब्दी में बनाया गया था।
८वीं से १४वीं शताब्दी तक, तांत्रिक परंपराएं प्रमुखता से बढ़ीं और पूरे भारत और उसके बाहर फली-फूलीं। [१३६] [१३७] [२१] [१३८] १०वीं शताब्दी तक, तांत्रिक अभ्यास के मुख्य तत्व परिपक्वता तक पहुँच चुके थे और शैव और बौद्ध संदर्भों में इसका अभ्यास किया जा रहा था। तंत्र की व्यापकता के कारण कुछ विद्वानों द्वारा इस अवधि को “तांत्रिक युग” के रूप में संदर्भित किया गया है। [१३९] इसके अलावा १०वीं शताब्दी तक, कई तांत्रिक ग्रंथ (जिन्हें आगम , संहिता और तंत्र कहा जाता है ) विशेष रूप से कश्मीर, नेपाल और बंगाल में लिखे जा चुके थे। [१४०] इस समय तक, तांत्रिक ग्रंथों का तमिल जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका था, और तांत्रिक प्रथाएं पूरे दक्षिण एशिया में फैल गई थीं। [१४१] तंत्र तिब्बत, इंडोनेशिया और चीन में भी फैल गया। गेविन फ्लड इस “तांत्रिक युग” का वर्णन इस प्रकार करता है:
तंत्रवाद इतना व्यापक रहा है कि ग्यारहवीं शताब्दी के बाद, शायद वैदिक श्रौत परंपरा को छोड़कर, सभी हिंदू धर्म इससे प्रभावित हैं। शैव , वैष्णव और स्मार्ट धर्म के सभी रूपों , यहां तक कि वे रूप जो तंत्रवाद से खुद को दूर करना चाहते थे, तंत्रों से प्राप्त तत्वों को अवशोषित करते थे। [१४१]
यद्यपि भारत का पूरा उत्तरी और हिमालयी हिस्सा तंत्र के विकास में शामिल था, कश्मीर एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण केंद्र था, शैव और बौद्ध दोनों और पैडौक्स के अनुसार कई प्रमुख तांत्रिक ग्रंथ वहां लिखे गए थे। [142] के अनुसार एलेक्सिस सैंडरसन , मध्ययुगीन कश्मीर के शैव तंत्र परंपराओं मुख्य रूप से द्वैतवादी शैव सिद्धांत और गैर dualist धर्मशास्त्र की तरह sakta प्रजातियों में पाया बीच विभाजित किया गया Trika , Krama और कौल । गैर-द्वैतवादियों ने आम तौर पर यौन और उल्लंघनकारी प्रथाओं को स्वीकार किया और उनका उपयोग किया, जबकि द्वैतवादियों ने ज्यादातर उन्हें खारिज कर दिया। [१४३] शैव तंत्र विशेष रूप से सफल रहा क्योंकि यह दक्षिण एशियाई राजाओं के साथ मजबूत संबंध बनाने में कामयाब रहा, जिन्होंने योद्धा देवी दुर्गा जैसे उग्र देवताओं की शक्ति (शक्ति) को अपनी शाही शक्ति बढ़ाने के तरीके के रूप में महत्व दिया । इन राजाओं ने शैव “शाही गुरुओं” के नेतृत्व में शाही अनुष्ठानों में भाग लिया, जिसमें उनका प्रतीकात्मक रूप से तांत्रिक देवताओं से विवाह हुआ और इस तरह वे शिव जैसे पुरुष देवताओं के सांसारिक प्रतिनिधि बन गए। शैव तंत्र विभिन्न प्रकार के संरक्षण और विनाश अनुष्ठानों को भी नियोजित कर सकता था जिनका उपयोग राज्य और राजा के लाभ के लिए किया जा सकता था। [144] तांत्रिक शैव, साथ ही द्वारा कश्मीर के राजाओं द्वारा अपनाया गया था Somavamshis की ओडिशा , Kalachuris , और Jejakabhukti के चंदेल (में बुंदेलखंड )। [१४५] कंबोडियाई खमेर साम्राज्य से राज्य के समर्थन का भी प्रमाण है । [१४६] जैसा कि सैमुअल ने उल्लेख किया है, देवी-देवताओं के बढ़ते चित्रण के बावजूद, ये तांत्रिक परंपराएं ज्यादातर “पुरुष-निर्देशित और पुरुष-नियंत्रित” थीं। [147]
“तांत्रिक युग” के दौरान, बौद्ध तंत्र को महायान बौद्ध मुख्यधारा द्वारा अपनाया गया था और नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन किया गया था , जहां से यह तिब्बत और चीन, कोरिया और जापान के पूर्वी एशियाई राज्यों में फैल गया। इस नए तांत्रिक बौद्ध धर्म को पाल राजवंश (8वीं-12वीं शताब्दी) का समर्थन प्राप्त था जिसने इन शिक्षा केंद्रों का समर्थन किया। [१४८] बाद के खमेर राजाओं और इंडोनेशियाई श्रीविजय साम्राज्य ने भी तांत्रिक बौद्ध धर्म का समर्थन किया। सैमुअल के अनुसार, जबकि बाद में तिब्बती बौद्ध मठवासी संदर्भों में यौन और उल्लंघनकारी प्रथाओं को ज्यादातर प्रतीकात्मक रूप में (या दृश्य के माध्यम से) किया गया था, ऐसा लगता है कि आठवीं से दसवीं शताब्दी के भारतीय संदर्भ में, वे वास्तव में किए गए थे। [149]
१०वीं और ११वीं शताब्दी में, शैव और बौद्ध तंत्र दोनों ही अधिक प्रसिद्ध, दार्शनिक और मुक्ति-उन्मुख धर्मों में विकसित हुए। इस परिवर्तन ने बाहरी और अतिक्रमणकारी अनुष्ठानों से आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने पर केंद्रित एक अधिक आंतरिक योग अभ्यास की ओर एक कदम देखा। इस पुनर्रचना ने तांत्रिक धर्मों को अन्य समूहों द्वारा हमले के लिए बहुत कम खुला बना दिया। शैव धर्म में, यह विकास अक्सर कश्मीरी गुरु अभिनवगुप्त (सी। 950 – 1016 सीई) और उनके अनुयायियों के साथ जुड़ा हुआ है , साथ ही आंदोलनों जो उनके काम से प्रभावित थे, जैसे श्री विद्या परंपरा (जो दक्षिण भारत तक फैली हुई थी , और इसे “उच्च” तंत्र के रूप में संदर्भित किया गया है)। [150]
बौद्ध धर्म में, तंत्र का यह नामकरण बौद्ध मठों द्वारा तंत्र को अपनाने के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इसे बौद्ध महायान शैक्षिक ढांचे के भीतर शामिल करने की मांग की थी। बौद्ध तंत्रों को लिखा गया और अभयकरगुप्त जैसे विद्वानों ने उन पर भाष्य लिखे। एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति, बंगाली शिक्षक अतिश ने एक ग्रंथ लिखा, जिसने तंत्र को जागृति के लिए एक स्नातक महायान पथ, बोधिपथप्रदीप की परिणति के रूप में रखा । उनके विचार में, व्यक्ति को पहले गैर-तांत्रिक महायान का अभ्यास शुरू करना चाहिए, और फिर बाद में तंत्र के लिए तैयार हो सकता है। यह प्रणाली गेलुग जैसे कुछ तिब्बती बौद्ध स्कूलों में तांत्रिक अभ्यास का आदर्श बन गई । तिब्बत में, तंत्र के उल्लंघनकारी और यौन अभ्यास बहुत कम केंद्रीय हो गए और तांत्रिक अभ्यास को केवल एक छोटे से कुलीन समूह के लिए उपयुक्त माना जाता था। [१५१] इस बाद की अवधि के दौरान भी नए तंत्रों की रचना जारी रही, जैसे कि कालचक्र (सी। ११वीं शताब्दी), जो बौद्धों और गैर-बौद्धों को समान रूप से परिवर्तित करने और उन्हें इस्लाम के खिलाफ एकजुट करने से संबंधित प्रतीत होता है। कालचक्र यौन योग सिखाता है, लेकिन यह भी चेतावनी देता है कि शुरुआती लोगों को अशुद्ध पदार्थों के सेवन का अभ्यास शुरू न करें, क्योंकि यह केवल उन्नत योगियों के लिए है। यह तंत्र भी अतिक्रमणकारी प्रथाओं के प्रभाव को कम करना चाहता है, क्योंकि यह तांत्रिकों को बाहरी रूप से अपने देश के रीति-रिवाजों का पालन करने की सलाह देता है। [१५२]
इस अवधि के दौरान एक और प्रभावशाली विकास तांत्रिक योगिक तकनीकों का संहिताकरण था जो बाद में हठ योग के रूप में जाना जाने वाला अलग आंदोलन बन गया । जेम्स मैलिसन के अनुसार, हठ योग के लिए मूल “स्रोत पाठ” वज्रयान बौद्ध अमृतसिद्धि (11 वीं शताब्दी सीई) है जो महासिद्ध विरुप को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस पाठ को बाद में शैव योगिक परंपराओं (जैसे नाथ ) द्वारा अपनाया गया और उनके ग्रंथों में उद्धृत किया गया है। [१५३] [१५४]
हिंदू तंत्र की एक और परंपरा वैष्णवों के बीच विकसित हुई , इसे पंचरात्र आगम परंपरा कहा गया । इस परंपरा ने शैवों और बौद्धों द्वारा ग्रहण किए गए आक्रामक और यौन तत्वों से परहेज किया। [119] वहाँ भी एक छोटे तांत्रिक के साथ जुड़े परंपरा है सूर्य , सूर्य देव। ऐसा लगता है कि जैन धर्म ने भी सौर परंपरा के आधार पर यक्ष और यक्षिणियों पर आधारित अनुष्ठानों के साथ एक पर्याप्त तंत्र कोष विकसित किया है । हालाँकि, इस जैन तंत्र का उपयोग मुख्य रूप से सुरक्षा जैसे व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया था। इन जैन तंत्रों की पूरी पांडुलिपियां नहीं बची हैं। [१५५] [१५६] ऐसा लगता है कि जैनियों ने भी तंत्र के कुछ सूक्ष्म शरीर अभ्यासों को अपनाया है, लेकिन यौन योग को नहीं। [128] श्वेताम्बर विचारक Hemacandra (सी। 1089-1172) इस तरह के चक्रों पर आंतरिक ध्यान, जो कौल और नाथ प्रभावों को धोखा के रूप में बड़े पैमाने पर तांत्रिक प्रथाओं, चर्चा करता है। [१५७]
स्वागत और बाद के घटनाक्रम
१७वीं शताब्दी की पांडुलिपि से, भैरवी और शिव का एक चारण मैदान में चित्रण।
ऐसा लगता है कि तंत्र की उपयुक्तता के बारे में कुछ बहस हुई है। हिंदुओं में, अधिक रूढ़िवादी वैदिक परंपराओं से संबंधित लोगों ने तंत्रों को खारिज कर दिया। इस बीच, तांत्रिकों ने वैदिक विचारों को अपनी प्रणालियों में शामिल किया, जबकि तंत्रों को उच्चतर, अधिक परिष्कृत समझ के रूप में माना। [१५५] इस बीच, कुछ तांत्रिकों ने तंत्रों को वेदों से श्रेष्ठ माना, जबकि अन्य ने उन्हें पूरक माना जैसे कि उमापति, जिन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया है: “वेद गाय है, सच्चा आगम इसका दूध है।” [१५८]
सैमुअल के अनुसार, महान अद्वैत दार्शनिक शंकर (9वीं शताब्दी) को “उनकी जीवनी, शंकरविजय में चित्रित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के तांत्रिक चिकित्सकों के दृष्टिकोण की निंदा करते हैं और उन्हें तर्क या आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से हराते हैं।” यह भी कहा जाता है कि उन्होंने उग्र देवी-देवताओं को सौम्य महिला देवताओं के साथ बदलने के लिए प्रोत्साहित किया, और इस प्रकार श्री विद्या परंपरा को बढ़ावा दिया (जो एक शांतिपूर्ण और प्यारी देवी, त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करती है )। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि शंकर ने वास्तव में तंत्र के खिलाफ अभियान चलाया था, उन्हें पारंपरिक रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिन्होंने हिंदू धर्म को अतिक्रमणकारी और विरोधी तांत्रिक प्रथाओं से शुद्ध किया। [१५९]
१३वीं शताब्दी के द्वैत वेदांत दार्शनिक माधवाचार्य ने भारतीय दर्शन और प्रथाओं के तत्कालीन मौजूदा प्रमुख विद्यालयों पर प्रचुर टिप्पणियां लिखीं, और १०वीं शताब्दी के अभिनवगुप्त के कार्यों का हवाला दिया , जिन्हें एक प्रमुख और प्रभावशाली तंत्र विद्वान माना जाता था। [१६०] हालांकि, माधवाचार्य तंत्र का उल्लेख एक अलग, विशिष्ट धार्मिक या अनुष्ठान-संचालित अभ्यास के रूप में नहीं करते हैं। २०वीं सदी के शुरुआती भारतीय विद्वान पांडुरंग वामन केन ने अनुमान लगाया कि माधवाचार्य ने तंत्र की उपेक्षा की क्योंकि इसे निंदनीय माना जा सकता है। इसके विपरीत, पैडौक्स का सुझाव है कि तंत्र 13 वीं शताब्दी तक इतना व्यापक हो गया होगा कि “इसे एक विशिष्ट प्रणाली के रूप में नहीं माना जाता था।” [१६०]
हिंदू तंत्र, जबकि कुछ सामान्य आबादी द्वारा अभ्यास किया जाता था, अंततः 15 वीं शताब्दी के बाद से पूरे भारत में फैले अधिक लोकप्रिय भक्ति आंदोलनों से प्रभावित हुआ । सैमुअल के अनुसार, “धर्म की ये नई भक्ति शैली, सर्वोच्च उद्धारकर्ता-देवता, चाहे शैव या वैष्णव, को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करने पर जोर देने के साथ, मुस्लिम शासन के तहत गैर-मुस्लिम समूहों की निम्न भूमिका के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित किया गया था।” [१६१] हालांकि अधिकांश शैव तपस्वियों के बीच शैव तंत्र एक महत्वपूर्ण अभ्यास बना रहा। [१६२] तांत्रिक परंपराएं कुछ क्षेत्रों में भी जीवित रहीं , जैसे राजस्थान के नाथों में, दक्षिण भारत की श्री विद्या परंपरा में और बंगाली बाउल में । [१६१]
बौद्ध धर्म में, जबकि नालंदा और विक्रमशिला के महान महायान प्रतिष्ठानों में तंत्र स्वीकार किया गया और हिमालयी क्षेत्रों में फैल गया, इसने अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में भी गंभीर झटके का अनुभव किया। बर्मा में, उदाहरण के लिए, राजा अनवरथ (1044-1077) के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तांत्रिक ” अरी ” भिक्षुओं को भंग कर दिया था। जैसे ही थेरवाद बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में प्रभावी हो गया, उन क्षेत्रों में तांत्रिक धर्म हाशिए पर चले गए। [१६३] श्रीलंका में, तांत्रिक बौद्ध धर्म को भी दुर्बल करने वाले झटके लगे। प्रारंभ में बड़ा अभयगिरी मठ एक ऐसा स्थान था जहां 8 वीं शताब्दी के दौरान वज्रयान की प्रथा फली-फूली। हालाँकि, अभयगिरी को भंग कर दिया गया था और पराक्रमबाहु I (११५३-११८६) के शासनकाल के दौरान रूढ़िवादी महाविहार संप्रदाय में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया था । [१६४]
१९वीं और २०वीं शताब्दी में हिंदू आधुनिकतावाद की अवधि के दौरान तंत्र के स्वागत के बारे में , सैमुअल लिखते हैं कि इस अवधि में “तांत्रिक संदर्भ से दूर योग प्रथाओं का एक क्रांतिकारी पुनर्मूल्यांकन हुआ।” सैमुअल ने नोट किया कि हिंदू हठ योग की उत्पत्ति एक शैव तांत्रिक संदर्भ में हुई थी,
उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्यवर्गीय भारत में प्रचलित तंत्र और उसकी यौन और जादुई प्रथाओं के बेहद नकारात्मक विचारों को देखते हुए, और आज भी काफी हद तक प्रचलित है, यह एक शर्मनाक विरासत थी। स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने योग के पुनर्निर्माण में बहुत प्रयास किए , आमतौर पर पतंजलि के योगसूत्र (डी मिशेलिस 2004) के चुनिंदा वेदांतिक पढ़ने के संदर्भ में । प्रयास काफी हद तक सफल रहा, और स्वास्थ्य और विश्राम के लिए योग के कई आधुनिक पश्चिमी चिकित्सकों को नाथ परंपरा की आंतरिक यौन प्रथाओं की तैयारी के रूप में इसके मूल कार्य के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है। [१६२]
आधुनिक बौद्ध तंत्र के संबंध में, यह आधुनिक भारत-तिब्बत बौद्ध धर्म में, विभिन्न जापानी परंपराओं जैसे शिंगोन और काठमांडू घाटी के नेवार बौद्ध धर्म में जीवित रहा है। [१६५] दक्षिण पूर्व एशिया में जादुई अर्ध-तांत्रिक परंपराएं भी हैं, जिन्हें कभी-कभी एसोटेरिक दक्षिणी बौद्ध धर्म कहा जाता है , हालांकि उन्हें “तांत्रिक” नहीं कहा जाता है और थेरवाद बौद्ध धर्म के राज्य समर्थित आधुनिकतावादी रूपों द्वारा हाशिए पर रखा गया है। [१६६]
तांत्रिक परंपराएं
हिंदू तंत्र
हिंदू धर्म के भीतर, तंत्र शब्द अक्सर एक पाठ को संदर्भित करता है, जो “तांत्रिक” हो भी सकता है और नहीं भी। इसके विपरीत, विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों को वास्तव में हमेशा तंत्र नहीं कहा जाता है (इसके बजाय उन्हें आगम, ज्ञान , संहिता, सिद्धांत, विद्या कहा जा सकता है )। [८३] [१६७] तांत्रिक उपनिषद भी हैं , जो देर से उपनिषद के साथ-साथ तांत्रिक पुराण (और तांत्रिक विचारों से प्रभावित पुराण) हैं। [१६८] इस प्रकार के ग्रंथों के अलावा, विभिन्न प्रकार के तांत्रिक ” शास्त्र ” (ग्रंथ) भी हैं जो “टिप्पणियां, पाचन, संकलन, मोनोग्राफ, भजनों का संग्रह या देवताओं के नाम, और मंत्र और मंत्रों पर काम कर सकते हैं। ” यद्यपि इस तांत्रिक साहित्य का अधिकांश भाग संस्कृत में है, अन्य भारतीय स्थानीय भाषाओं में भी लिखे गए हैं। जैसा कि पडौक्स ने उल्लेख किया है, इन तांत्रिक कार्यों का सबसे बड़ा हिस्सा शैव ग्रंथ हैं। [१६९]
तांत्रिक ग्रंथों और चिकित्सकों (“तांत्रिकों”) को अक्सर वैदिक ग्रंथों और वैदिक धर्म (“वैदिका”) का अभ्यास करने वालों के साथ तुलना की जाती है। इस गैर-वैदिक पथ को अक्सर मंत्रमार्ग (“मंत्रों का तरीका”) या तंत्रशास्त्र (“तंत्र शिक्षण”) कहा जाता था। इस द्विभाजन पर सबसे प्रसिद्ध टिप्पणियों में से एक है कुल्लुका भट्ट का मनुस्मृति पर १५वीं शताब्दी की अपनी टिप्पणी में बयान जिसमें कहा गया है कि रहस्योद्घाटन (श्रुति) दो गुना है – वैदिक और तांत्रिक। [१६७] हिंदू तांत्रिक शिक्षाओं को आम तौर पर एक दिव्य प्राणी (जैसे शिव, या देवी) से रहस्योद्घाटन के रूप में देखा जाता है, जिसे तांत्रिकों द्वारा मुक्ति के लिए अग्रणी प्राणियों में वेदों से श्रेष्ठ माना जाता है। उन्हें कलियुग के दौरान भी अधिक प्रभावी माना जाता है, जो बहुत जुनून (काम) का समय है। हालाँकि, अभिनवगुप्त जैसे तांत्रिक विचारक , तंत्र को श्रेष्ठ मानते हुए, वैदिक शिक्षाओं को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करते हैं, और इसके बजाय उन्हें निचले स्तर पर मान्य मानते हैं क्योंकि वे भी उसी स्रोत, सर्वोच्च देवत्व से प्राप्त होते हैं। [83] [170]
शैववाद, शक्तिवाद और वैष्णववाद के भीतर विभिन्न हिंदू तांत्रिक परंपराएं हैं। [१७१] इन विभिन्न परंपराओं के लिए विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के साथ कई तांत्रिक ग्रंथ हैं, जो आस्तिक द्वैतवाद से लेकर पूर्ण अद्वैतवाद तक हैं । [१७२] [१७३] डेविड बी ग्रे के अनुसार, “तांत्रिक परंपराओं के प्रसार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ट्रॉप्स में से एक वंश है, एक निर्बाध वंश के साथ शिक्षाओं का संचरण, गुरु से शिष्य तक, इसलिए तथाकथित guruparaṃparā । ” [८३] ये विभिन्न परंपराएं आपस में इस बात पर भी भिन्न हैं कि वे कितने विधर्मी और अतिक्रमणकारी हैं (वैदिक परंपरा के अनुसार)। चूंकि तांत्रिक अनुष्ठान इतने व्यापक हो गए थे, तंत्र के कुछ रूपों को अंततः कई रूढ़िवादी वैदिक विचारकों जैसे कि जयंत भट्ट और यमुनाचार्य द्वारा स्वीकार किया गया था, जब तक कि वे वैदिक शिक्षण और सामाजिक नियमों का खंडन नहीं करते थे। [१७४] काली केंद्रित जयद्रथयामाला जैसे तांत्रिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि तांत्रिक वैदिक सामाजिक नियमों का पालन सुविधा के लिए और अपने कबीले और गुरु के लाभ के लिए कर सकते हैं। [१७५] हालांकि, सभी वैदिक विचारकों ने तंत्र को स्वीकार नहीं किया। उदाहरण के लिए, कुमारिला भट्ट ने लिखा है कि किसी को तांत्रिकों से संपर्क नहीं करना चाहिए और न ही उनसे बात करनी चाहिए। [१७६]
शैव और शाक्त तंत्र:
Brihadishvara मंदिर , में एक शैव सिद्धांत मंदिर तमिलनाडु
देवी काली का नेपाली चित्रण
श्री, जिसे ललिता त्रिपुरासुंदरी (“तीन लोकों में सुंदर”), आदि पराशक्ति (सर्वोच्च सर्वोच्च ऊर्जा), कामेश्वरी (इच्छा की देवी) और अन्य नामों से भी जाना जाता है।
शैव तंत्र कहा जाता है Mantramārga , और अक्सर तपस्वी “Atimārga” परंपरा (जो भी शामिल है की तुलना में एक अलग शिक्षण होने के रूप में देखा जाता है Pāśupatas और कापालिक)। [८३] [१७७] शैव तंत्र के विभिन्न सिद्धांत, पाठ्य कक्षाएं और स्कूल हैं, जो अक्सर अलग-अलग तरीकों से शाक्त परंपरा के साथ ओवरलैप करते हैं।
शैव सिद्धांत परंपरा परंपरा जल्द से जल्द शैव तंत्र स्कूल और पुजारियों द्वारा किया जाता सार्वजनिक अनुष्ठानों की विशेषता थी। उनके कुछ ग्रंथ, जैसे निश्वासतत्त्वसंहिता , पांचवीं शताब्दी के हैं। [८३] उनके शास्त्र (शैव आगम) और बुनियादी सिद्धांत भी अन्य परंपराओं द्वारा एक सामान्य शैव सिद्धांत के रूप में साझा किए जाते हैं और उनके कई संस्कार शैव तंत्र के अन्य स्कूलों में भी उपयोग किए जाते हैं। [१७७] शैव सिद्धांत आगमों के नुस्खे और अनुष्ठानों का आमतौर पर दक्षिण भारत में शैव मंदिरों द्वारा पालन किया जाता है और वे ज्यादातर रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद के अनुकूल हैं, जिनमें भयानक देवताओं और पशु बलि का अभाव है। [१७८]
दूसरी ओर Mantrapīṭha परंपरा, Svacchanda पूजा भैरव , शिव का एक भयानक रूप को “Aghora” ( “डरावना नहीं”) में जाना जाता है। यह परंपरा खोपड़ी के पालन ( कपलव्रत ) को बढ़ावा देती है , यानी खोपड़ी, एक खोपड़ी कर्मचारी (खतवंगा) लेकर और श्मशान घाट में पूजा करना। [179] कापालिक संन्यासियों में से एक समकालीन समूह रहे हैं Aghoris ।
विभिन्न परंपराएं भी हैं जिन्हें “विद्यापीठ” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस परंपरा के ग्रंथों में योगिनी या शाकिनियों के रूप में जानी जाने वाली देवी की पूजा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसमें धर्म-विरोधी प्रथाएं शामिल हैं जो कि चारण आधार और कामुकता से संबंधित हैं। [८३] शक्ति तंत्र की ये देवी-केंद्रित परंपराएं ज्यादातर “वाम” धारा ( वामचार ) की हैं और इस प्रकार इन्हें अधिक विधर्मी माना जाता है। [180]
विभिन्न विद्यापीठ परंपराएं हैं, जो एक द्विध्रुवीय, उभयलिंगी देवत्व पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो समान भागों में पुरुष और महिला, शैव और शाक्त हैं। Yamalatantras Kapalini, खोपड़ी की देवी के साथ भैरव पूजा करते हैं। देवी केंद्रित परंपराओं को कुलमार्ग (कुलों का पथ) के रूप में जाना जाता है , जो देवी-देवताओं के कुलों और उनके शक्ति तंत्रों का जिक्र करते हैं , जो 9वीं शताब्दी के आसपास स्थापित हो सकते हैं। इसमें यौन अनुष्ठान, संगीन प्रथाएं, शराब की रस्म खपत और आत्मा के कब्जे का महत्व शामिल है । इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित विभिन्न उप-परंपराएं शामिल हैं, जैसे कि त्रिक वंश (जो देवताओं की तिकड़ी की पूजा करता है: पारा, परापारा, और अपरा), उग्र देवी गुह्यकाली की परंपरा, क्रमा परंपरा, देवी पर ध्यान केंद्रित करती है। काली , कुब्जिका पंथ, और दक्षिणी परंपरा जो सुंदर देवी कामेश्वरी या त्रिपुरासुंदरी की पूजा करती है। [83] [180]
१०वीं शताब्दी के दौरान, कश्मीर शैववाद के समकालिक नॉनडुअल स्कूल का विकास हुआ। एलेक्सिस सैंडरसन के अनुसार, यह परंपरा द्वैतवादी और अधिक रूढ़िवादी शैव सिद्धांत और त्रिक और क्रमा की अद्वैतवादी परंपराओं के बीच टकराव से उत्पन्न हुई। डेविड बी ग्रे के अनुसार, इस स्कूल ने इन दोनों परंपराओं के तत्वों को एकीकृत किया, “अंतिम परिणाम एक अद्वैतवादी प्रणाली थी जिसमें आक्रामक तत्वों को आंतरिक रूप दिया गया था और इसलिए रूढ़िवादी के लिए कम आक्रामक हो गया।” [83]
कश्मीर शैववाद के दार्शनिक, विशेष रूप से अभिनवगुप्त ( सी । 975-1025 सीई) और उनके छात्र जयरथ, हिंदू तंत्र पर लिखने वाले कुछ सबसे प्रभावशाली दार्शनिक हैं। [१८१] इन विचारकों ने विभिन्न देवी और शिव वंशों और दर्शनों को एक व्यापक और प्रभावशाली धार्मिक व्यवस्था में संश्लेषित किया। डेविड व्हाइट के अनुसार, अभिनवगुप्त ने “अपनी कई प्रथाओं को एक प्रकार के ध्यानपूर्ण तपस्या के रूप में उभारा, सौंदर्यीकरण और शब्दार्थ किया, जिसका उद्देश्य एक उत्कृष्ट विषय का एहसास करना है।” [८३] इस प्रकार, उनके काम ने विद्यापीठ वंश की मौलिक रूप से विरोधी विरोधी प्रथाओं को ध्यान अभ्यास में बदल दिया। [83]
अंतिम प्रमुख शैव तांत्रिक परंपरा नाथ या “विभाजित-कान” कानफड़ा परंपरा है , जो 12 वीं या 13 वीं शताब्दी में उभरी थी। उन्होंने विभिन्न हठयोग ग्रंथों का निर्माण किया जो तांत्रिक योगों पर आधारित हैं। [83] [182]
जबकि शाक्त परंपराएं अलग-अलग तरीकों से विकसित होती रहीं, कभी-कभी अधिक लोकप्रिय और भक्तिपूर्ण दिशा में, उनमें से कई आज विभिन्न तांत्रिक तत्वों को बरकरार रखती हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय शाक्त तंत्र परंपराएं आज दक्षिणी कौला संचरण हैं, जो सुंदर देवी श्री ( श्रीकुला ) या ललिता त्रिपुरासुंदरी और उत्तरी और पूर्वी संचरण पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो क्रूर देवी काली ( कालीकुला ) पर केंद्रित हैं । [८३] दक्षिणी प्रसारण ने श्री विद्या परंपरा को जन्म दिया , जो दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण तांत्रिक धर्म है। यद्यपि यह कश्मीर शैववाद से अपनी अधिकांश दार्शनिक और सैद्धांतिक प्रणाली लेता है, यह आम तौर पर आक्रामक तत्वों से बचता है और रूढ़िवादी या “दाहिने हाथ” है। भास्करराय (18वीं शताब्दी) को इस परंपरा का प्रमुख विचारक माना जाता है। [८३] [१८१] कालिकुल परंपरा पूर्व और दक्षिण भारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और काली भारत में एक लोकप्रिय देवी बनी हुई है, जो बहुत अधिक भक्ति का केंद्र है। [83]
वैष्णव
तंत्र से जुड़ी मुख्य वैष्णव परंपरा पंचरात्र है । इस परंपरा ने कई तांत्रिक ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें से अधिकांश खो गए हैं। हालांकि, यह संप्रदाय खुद को “तांत्रिक” के रूप में नहीं पहचानता है। [८३] दक्षिण भारत में अधिकांश वैष्णव मंदिरों की पूजा और अनुष्ठान इस परंपरा का पालन करते हैं, जो कि शैव सिद्धांत के समान है। पैडौक्स के अनुसार, “सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, वे ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता के करीब हैं (उनके कुछ सहयोगियों द्वारा गर्व से जोर दिया गया) और उनके मंत्र वास्तव में अक्सर वैदिक होते हैं।” [१८३]
डेविड बी ग्रे के अनुसार,
“मध्ययुगीन काल के दौरान बंगाल में एक और तांत्रिक वैष्णव परंपरा का उदय हुआ। सहजिया परंपरा के रूप में जाना जाता है , यह 16 वीं से 19 वीं शताब्दी के आसपास बंगाल में फली-फूली। इसने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिव्यता है, जो दिव्य युगल कृष्ण और उनकी पत्नी राधा का प्रतीक है। यह परंपरा एक वैष्णव धार्मिक ढांचे के भीतर पहले हिंदू और बौद्ध तांत्रिक प्रथाओं को एकीकृत करती है।” [83]
बौद्ध तंत्र
पूरे एशिया में विभिन्न बौद्ध तांत्रिक परंपराएँ हैं जिन्हें अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है जैसे वज्रयान, गुप्त मंत्र, मंत्रयान आदि। [184] [185] [186] भारत और तिब्बती बौद्ध परंपरा में प्रमुख हो गया है तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र। [१८४] यह पहली बार ८वीं शताब्दी में तिब्बत में फैला और तेजी से प्रमुखता तक पहुंचा। [८३] तिब्बती बौद्ध तांत्रिक शिक्षाओं को हाल ही में तिब्बती प्रवासियों द्वारा पश्चिमी दुनिया में फैलाया गया है । नेपाली नेवार बौद्ध धर्म इस बीच काठमांडू घाटी में नेवार लोगों द्वारा अभी भी प्रचलित है । परंपरा संस्कृत ग्रंथों का एक सिद्धांत बनाए रखती है, जो अभी भी ऐसा करने वाली एकमात्र बौद्ध तांत्रिक परंपरा है।
५वीं से ८वीं शताब्दी तक विकसित बौद्ध तांत्रिक प्रथाओं और ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया गया था और चीनी बौद्ध सिद्धांत के साथ-साथ दुनहुआंग पांडुलिपियों में भी संरक्षित हैं । [१८४] [१८७] चीनी गूढ़ बौद्ध धर्म तांग राजवंश और सांग राजवंश के दौरान अत्यधिक प्रभावशाली था । मिंग राजवंश के दौरान , चीनी गूढ़ बौद्ध धर्म सहित विभिन्न चीनी बौद्ध परंपराएं काफी हद तक एक साथ जुड़ गईं। इसके बाद, चीनी तांत्रिक प्रथाओं और शिक्षाओं को अवशोषित कर लिया गया और अन्य बौद्ध परंपराओं जैसे चान , तियानताई और हुआयन में विलय कर दिया गया । आधुनिक चीनी बौद्ध धर्म में, गूढ़ परंपराओं को कई तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से पारित किया जाता है और अभ्यास किया जाता है जैसे कि यूनिवर्सल क्रॉसिंग (普渡 Pdù) भूखे भूतों के लिए संस्कार और सम्राट लियांग पश्चाताप समारोह, साथ ही साथ तांत्रिक मंत्रों का पाठ जैसे कि Cundī धरणी , Cintamanicakra मंत्र और Shurangama मंत्र । [१८८] गूढ़ प्रथाएं कोरिया और जापान में भी फैल गईं, जहां यह आधुनिक समय में शिंगोन नामक एक स्वतंत्र परंपरा के रूप में जीवित है । [83]
अन्य धर्म
हिंदू और बौद्ध तांत्रिक परंपराओं ने जैन धर्म, सिख धर्म , तिब्बती बॉन परंपरा, दाओवाद , शिंटो , सूफी इस्लाम और पश्चिमी ” नए युग ” आंदोलन जैसे कई अन्य धर्मों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया । [१८९] [१९०] [१९१]
सिख साहित्य में, शक्ति और देवी श्रद्धा से संबंधित विचार , विशेष रूप से दशम ग्रंथ में, गुरु गोबिंद सिंह को जिम्मेदार ठहराया , बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में पाए जाने वाले तंत्र विचारों से संबंधित हैं। [१९२]
एलेन गॉफ कहते हैं, जैन पूजा के तरीके संभवतः शक्तिवाद के विचारों से प्रभावित थे , और यह ऋषि-मंडल के तांत्रिक आरेखों द्वारा प्रमाणित है जहां तीर्थंकरों को चित्रित किया गया है। [१९३] जैन धर्म के भीतर तांत्रिक परंपराएं मौखिक मंत्र या मंत्र का उपयोग करती हैं , और अनुष्ठानों को पुनर्जन्म क्षेत्र के लिए योग्यता अर्जित करने के लिए माना जाता है। [१९४]
आचरण
तांत्रिक साहित्य के मुख्य तत्वों में से एक है अनुष्ठान [१ ९५] [नोट ५] एक सुसंगत प्रणाली के बजाय, तंत्र विभिन्न स्रोतों से प्रथाओं और विचारों का एक संग्रह है। जैसा कि सैमुअल लिखते हैं, तांत्रिक परंपराएं “विभिन्न कारकों और घटकों की एक किस्म का संगम हैं।” इन तत्वों में शामिल हैं: मंडल, मंत्र, आंतरिक यौन योग अभ्यास, उग्र पुरुष और महिला देवता, श्मशान भूमि प्रतीक, साथ ही भारतीय दर्शन से अवधारणाएं। [१९६]
आंद्रे पैडौक्स ने नोट किया कि विद्वानों के बीच इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि तंत्र के लिए कौन से तत्व विशेषता हैं, और न ही ऐसा कोई पाठ है जिसमें वे सभी तत्व शामिल हैं। [१९७] साथ ही, उनमें से अधिकतर तत्व गैर-तांत्रिक परंपराओं में भी पाए जा सकते हैं। [१९७] इस शब्द द्वारा कवर किए गए समुदायों की विस्तृत श्रृंखला के कारण, निश्चित रूप से तांत्रिक प्रथाओं का वर्णन करना समस्याग्रस्त है। हालांकि, कई तांत्रिक परंपराओं द्वारा साझा की जाने वाली प्रथाओं और तत्वों के सेट हैं, और इस प्रकार उनके बीच एक पारिवारिक समानता संबंध स्थापित किया जा सकता है।
विभिन्न विद्वान तंत्र की विभिन्न मुख्य विशेषताएं देते हैं। उदाहरण के लिए, डेविड एन. लोरेंजेन लिखते हैं कि तंत्र विभिन्न “शैमैनिक और योगिक” प्रथाओं, देवी-देवताओं की पूजा, कौल और कपालिका जैसे विशिष्ट स्कूलों के साथ-साथ तांत्रिक ग्रंथों को साझा करता है। [६५] इस बीच, क्रिस्टोफर वालिस, तांत्रिक विद्वान रामकण्ठ की परिभाषा के आधार पर, तंत्र की चार मुख्य विशेषताएं देते हैं: “१) हेरफेर के अनुष्ठान के तरीकों (पर्यावरण या स्वयं की जागरूकता के बारे में), २) गूढ़ दीक्षा की आवश्यकता (शास्त्रीय शिक्षाओं और प्रथाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए), 3) अभ्यास का एक दोहरा लक्ष्य: सोटेरिओलॉजिकल और सुपरमुंडन मुक्ति का एक (विभिन्न रूप से कल्पना की गई) और/या अन्य प्राणियों और किसी के पर्यावरण पर असाधारण शक्ति में से एक, और 4) दावा है कि इन तीनों को शास्त्रों में समझाया गया है जो कि भगवान ( आगम ) या बुद्ध ( बुद्धवचन ) के शब्द हैं ।” [१९८]
बौद्ध तंत्र के विद्वान एंथोनी जनजाति के अनुसार , तंत्र में निम्नलिखित परिभाषित विशेषताएं हैं: [199]
कर्मकांड की केंद्रीयता, विशेष रूप से देवताओं की पूजा
मंत्रों की केंद्रीयता
एक देवता के दर्शन और पहचान
दीक्षा, गूढ़ता और गोपनीयता की आवश्यकता
एक शिक्षक का महत्व (गुरु, आचार्य )
मंडलों का अनुष्ठान उपयोग ( Maala )
उल्लंघनकारी या एंटीनोमियन कार्य
शरीर का पुनर्मूल्यांकन
महिलाओं की स्थिति और भूमिका का पुनर्मूल्यांकन
अनुरूप सोच (सूक्ष्म ब्रह्मांडीय या स्थूल ब्रह्मांडीय सहसंबंध सहित)
नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं का पुनर्मूल्यांकन
तांत्रिक तकनीकों या आध्यात्मिक प्रथाओं ( साधना ) की एक विस्तृत श्रृंखला है जैसे: [200]
दक्षिणा : अपने शिक्षक को दान या उपहार
गुरु योग और गुरु भक्ति (भक्ति)
दीक्षा या अभिषेक : दीक्षा अनुष्ठान जिसमें शक्तिपात शामिल हो सकता है
श्वास तकनीक ( प्राणायाम ) और आसन ( आसन ) सहित योग , शरीर/मन में ऊर्जा को संतुलित करने के लिए नियोजित है।
मुद्रा , या हाथ के इशारे gesture
मंत्र : शब्दांश, शब्द और वाक्यांशों का पाठ करना
स्तुति के भजनों का गायन ( स्तव )
मंडल और यंत्र , ब्रह्मांड में काम कर रहे बलों के प्रतीकात्मक चित्र diagram
देवताओं के दर्शन और ध्यान में इन देवताओं की पहचान (देवता योग)
पूजा (पूजा अनुष्ठान) और भक्ति के अन्य रूप
पशु बलि सहित अनुष्ठान बलिदान
शराब, भांग , मांस और अन्य एंथोजेंस जैसे वर्जित पदार्थों का उपयोग ।
प्रायश्चित – यदि कोई पूजा गलत तरीके से की गई है तो एक प्रायश्चित अनुष्ठान किया जाता है
न्यासा , शरीर पर मंत्रों की स्थापना installing
अनुष्ठान शुद्धि (मूर्तियों की, किसी के शरीर की, आदि)
यात्रा : तीर्थयात्रा, जुलूस process
व्रत और समया : व्रत या प्रतिज्ञा, कभी-कभी उपवास जैसे तपस्या करने के लिए
सिद्धियों या अलौकिक शक्तियों का अधिग्रहण और उपयोग । के साथ जुड़े बाएं हाथ पथ तंत्र ।
गणचक्र : एक अनुष्ठानिक भोज जिसके दौरान एक पवित्र भोजन किया जाता है।
अनुष्ठान संगीत और नृत्य।
यौन योग : कर्मकांड यौन मिलन (एक वास्तविक शारीरिक पत्नी या एक कल्पित देवता के साथ)।
स्वप्न योग
पूजा और अनुष्ठान
गणेश प्रतिमा के सामने एक पुजारी , बृहदीश्वर शिव मंदिर
हिंदू तंत्र में पूजा या पूजा वैदिक रूपों से कुछ अलग है। जबकि यज्ञ की वैदिक प्रथा में कोई मूर्ति, मंदिर और प्रतीकात्मक कला नहीं है, तंत्र में वे पूजा के महत्वपूर्ण साधन हैं। [201]
द्वैतवादी शैव सिद्धांत में अनुष्ठान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो पैडौक्स के अनुसार “आमतौर पर अनुष्ठानों की अधिकता की विशेषता है, जो आवश्यक रूप से मंत्रों के साथ होते हैं। ये अनुष्ठान मानसिक रूप से कल्पना और अनुभवी छवियों के एक नाटक के रूप में कार्यों का इतना उत्तराधिकार नहीं हैं, सभी तांत्रिक परंपराओं के लिए एक सामान्य स्थिति, जहां संस्कार, ध्यान और योग रचनात्मक पहचान कल्पना में अभ्यास हैं।” इन अनुष्ठानों के पीछे सिद्धांत यह विचार है कि सभी मनुष्यों में एक मौलिक अशुद्धता (माला) होती है जो उन्हें पुनर्जन्म के लिए बाध्य करती है। इस अशुद्धता को कर्मकांड (उचित ज्ञान के साथ) द्वारा दूर किया जा सकता है। इस पथ का प्रारंभिक चरण दीक्षा (दीक्षा) का अनुष्ठान है, जो मृत्यु पर भविष्य की मुक्ति के द्वार खोलता है। [२०२]
गैर-द्वैतवादी और अतिक्रमणकारी (या “बाएं हाथ”) परंपराओं में जैसे काली पंथ और त्रिक संप्रदाय, अनुष्ठान और पूजा में कुछ बाएं हाथ के पथ तत्व शामिल हो सकते हैं जो अधिक रूढ़िवादी परंपराओं में नहीं पाए जाते हैं। इन उल्लंघनकारी तत्वों में खोपड़ी और अन्य मानव हड्डी के औजार (कपालिका व्रत के हिस्से के रूप में), भैरव, कुबजिका और काली जैसे उग्र देवताओं का उपयोग शामिल है, जिनका उपयोग ध्यान दृश्यों के हिस्से के रूप में किया गया था, देवताओं (अवेसा) द्वारा अनुष्ठान का अधिकार, यौन संस्कार और देवता (साथ ही उपभोग करने वाले) को कुछ अशुद्ध पदार्थ जैसे मांस, शराब और यौन तरल पदार्थ चढ़ाते हैं। [२०३] पादौक्स इस प्रकार के उल्लंघनकारी प्रथाओं की व्याख्या करता है:
कर्मकांड और मानसिक तल पर, अतिक्रमण एक अनिवार्य गुण था जिसके द्वारा अद्वैतवादी तांत्रिक परंपराएं खुद को अन्य परंपराओं से अलग करती थीं – इतना अधिक कि उन्होंने “अद्वैतवादी अभ्यास” (अद्वैतकार) शब्द का इस्तेमाल कौला के उल्लंघनकारी प्रथाओं को अस्वीकृति के रूप में करने के लिए किया था। ब्राह्मणवादी समाज में शुद्ध और अशुद्ध के द्वैत (द्वैत) का। आइए यह भी ध्यान दें कि अद्वैतवादी शैव प्रणालियों के लिए, योगिनियाँ केवल आत्माओं की दुनिया में सक्रिय नहीं थीं; वे मनुष्यों में भी मौजूद शक्तियाँ थीं – उनकी इंद्रियों की मालकिन, उनके प्रभावों को नियंत्रित करने वाली, जिन्होंने इस दिव्यता के माध्यम से एक तीव्रता और अलौकिक आयाम प्राप्त किया। इसने उन्हें अपनी व्यक्तिगत चेतना को अनंत दिव्य चेतना के साथ पहचानने में मदद की, इस प्रकार उन्हें यौन स्तर को पार करने में भी मदद मिली। [२०४]
बौद्ध और शैव दोनों संदर्भों में, यौन प्रथाओं को अक्सर आनंद के उपयोग के माध्यम से किसी की चेतना का विस्तार करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। [२०४]
अनुष्ठान के संबंध में शैव सिद्धांत और त्रिक जैसे गैर-द्वैतवादी स्कूलों के बीच एक मौलिक दार्शनिक असहमति भी है। शैव सिद्धांत में, केवल अनुष्ठान “जन्मजात अशुद्धियों” ( अनवमाला ) को दूर कर सकता है जो व्यक्तिगत आत्माओं को बांधते हैं, हालांकि अनुष्ठान को उनकी प्रकृति और उद्देश्य की समझ के साथ-साथ भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। त्रिक विचारधारा (विशेषकर अभिनवगुप्त के कार्य) की दृष्टि में , केवल ज्ञान (ज्ञान ) जो हमारे वास्तविक स्वरूप की “मान्यता” ( प्रत्याभिज्ञ ) है, मुक्ति की ओर ले जाता है। पैडौक्स के अनुसार, “यह भी, बारीकियों के साथ, पंचरात्र और अन्य वैष्णव तांत्रिक परंपराओं की स्थिति है।” [205]
योग, मंत्र, ध्यान
एक ध्यान करने वाले शिव पार्वती के पास जाते हैं
तांत्रिक योग सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सन्निहित अभ्यास है, जिसे एक दैवीय गूढ़ संरचना के रूप में देखा जाता है। जैसा कि पैडौक्स ने उल्लेख किया है, तांत्रिक योग एक “रहस्यवादी शरीर विज्ञान” का उपयोग करता है जिसमें विभिन्न मनोदैहिक तत्व शामिल होते हैं जिन्हें कभी-कभी ” सूक्ष्म शरीर ” कहा जाता है । इस काल्पनिक आंतरिक संरचना में चक्र (“पहिए”), नाड़ियाँ (“चैनल”), और ऊर्जाएँ (जैसे कुंडलिनी, चांडाली, विभिन्न प्राण और महत्वपूर्ण हवाएँ, आदि) शामिल हैं। तांत्रिक शरीर को ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म प्रतिबिंब माना जाता है, और इस प्रकार इसे देवी-देवताओं के रूप में देखा जाता है। [२०६] पैडौक्स के अनुसार, “योगिक शरीर की आंतरिक छवि” लगभग सभी ध्यान और तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए एक मौलिक तत्व है। [207]
मंत्रों का प्रयोग तांत्रिक साधना के सबसे सामान्य और व्यापक तत्वों में से एक है। उनका उपयोग अनुष्ठानों के साथ-साथ विभिन्न ध्यान और योग प्रथाओं के दौरान भी किया जाता है। मंत्र पाठ ( जप ) का अभ्यास अक्सर न्यासा (“मंत्र जमा करना”), मुद्रा (“मुहरें”, यानी हाथ के इशारे) और जटिल दृश्यों के साथ किया जाता है जिसमें दैवीय प्रतीकों, मंडलों और देवताओं को शामिल किया जाता है। न्यासा में मंत्र का जाप करते हुए शरीर के विभिन्न हिस्सों को छूना शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह देवता को योगियों के शरीर से जोड़ता है और शरीर को देवता के शरीर में बदल देता है। [२०८]
मंत्रों को अक्सर तांत्रिक ध्यान के हिस्से के रूप में योगी के शरीर के भीतर स्थित होने के रूप में भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए, “योगिनी हार्ट” तंत्र में, एक श्री विद्या पाठ, योगी को मूलाधार चक्र में देवता के मंत्र के पांच अक्षरों (हा सा का ला ह्रीं) की कल्पना करने का निर्देश दिया गया है। पाँच अक्षरों का अगला सेट (हा सा का हा ला ह्रीम) हृदय चक्र में और तीसरा समूह (सा का ला ह्रीम) भौंहों के बीच के चक्र में देखा जाता है। योगी को आगे एचआरआईएम शब्दांश के अंत में एम ध्वनि के उच्चारण को लंबा करने का निर्देश दिया जाता है, एक अभ्यास जिसे नाडा (ध्वनि कंपन) कहा जाता है। यह अभ्यास विभिन्न सूक्ष्म चरणों से गुजरता है जब तक कि यह निरपेक्ष के मौन में विलीन नहीं हो जाता। [209]
तांत्रिक योग में पाया जाने वाला एक अन्य सामान्य तत्व दूरदर्शी ध्यान का उपयोग है जिसमें तांत्रिक देवता (या देवताओं) की दृष्टि या छवि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और कुछ मामलों में खुद को देवता के रूप में और अपने स्वयं के शरीर को देवता के शरीर के रूप में कल्पना करते हैं। . [२१०] अभ्यासी दृश्यावलोकन का उपयोग कर सकता है , एक देवता के साथ इस हद तक पहचान कर सकता है कि आकांक्षी इष्ट-देव (या ध्यान देवता ) “बन जाता है” । अन्य ध्यानों में, देवताओं को तांत्रिक के शरीर के अंदर होने की कल्पना की जाती है। उदाहरण के लिए, अभिनवगुप्त के तंत्रलोक (अध्याय 15) में, एक त्रिशूल (सिर के ऊपर स्थित) के तीन नुकीले सिरों पर देवी (परा, परा, और अपरा) की त्रिक “त्रिमूर्ति” की कल्पना की जाती है। शेष त्रिशूल को योगी के शरीर की केंद्रीय धुरी के साथ चित्रित किया गया है, जिसके सिर में शिव की धधकती लाश दिखाई दे रही है। [२११]
मंडल और यंत्र
दस महाविद्याओं के साथ श्री यंत्र आरेख । त्रिकोण शिव और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं ; सांप स्पंद और कुंडलिनी का प्रतिनिधित्व करता है ।
यंत्र रहस्यमय चित्र हैं जिनका उपयोग तांत्रिक ध्यान और अनुष्ठान में किया जाता है। वे आमतौर पर शिव, शक्ति या काली जैसे विशिष्ट हिंदू देवताओं से जुड़े होते हैं । इसी तरह, पूजा में किसी देवता से जुड़े यंत्र या मंडल पर ध्यान केंद्रित करना शामिल हो सकता है । [२१२]
डेविड गॉर्डन व्हाइट के अनुसार , ज्यामितीय मंडल तंत्र के प्रमुख तत्व हैं। [२१३] उनका उपयोग कई तांत्रिक विचारों और अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ ध्यान केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है। मंडल प्रतीकात्मक रूप से “उत्कृष्ट-अभी-आसन्न” स्थूल जगत और सांसारिक मानव अनुभव के सूक्ष्म जगत के बीच पत्राचार का संचार करते हैं। [२१३] देवत्व (या प्रमुख बुद्ध) को अक्सर मंडल के केंद्र में चित्रित किया जाता है, जबकि अभ्यासी सहित अन्य सभी प्राणी, इस केंद्र से विभिन्न दूरी पर स्थित होते हैं। [२१३] मंडलों ने मध्यकालीन सामंती व्यवस्था को भी प्रतिबिंबित किया , जिसके केंद्र में राजा था। [२१४]
मंडल और यंत्रों को विभिन्न तरीकों से चित्रित किया जा सकता है, चित्रों, कपड़े पर, तीन आयामी रूप में, रंगीन रेत या पाउडर आदि से बना होता है। तांत्रिक योग में अक्सर मंडल या यंत्र का मानसिक दृश्य शामिल होता है। यह आमतौर पर एक तांत्रिक साधना (अभ्यास) के हिस्से के रूप में मंत्र पाठ और अन्य अनुष्ठान क्रियाओं के साथ जोड़ा जाता है।
सेक्स और कामुकता
जबकि तंत्र में विचारों और प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है जो हमेशा एक यौन प्रकृति के नहीं होते हैं, फ्लड और पैडौक्स दोनों ध्यान देते हैं कि पश्चिम में, तंत्र को अक्सर एक प्रकार का अनुष्ठान सेक्स या आध्यात्मिक योगिक कामुकता माना जाता है । [२१५] [२१६] [२१७] पैडौक्स के अनुसार, “यह एक गलतफहमी है, हालांकि तंत्र में सेक्स का स्थान वैचारिक रूप से आवश्यक है, लेकिन क्रिया और अनुष्ठान में हमेशा ऐसा नहीं होता है।” पैडौक्स आगे नोट करते हैं कि जबकि यौन प्रथाएं मौजूद हैं और जहां कुछ तांत्रिक समूहों द्वारा उपयोग किया जाता है, उन्होंने “जब तंत्र अन्य बड़े सामाजिक समूहों में फैल गया तो उन्होंने अपना प्रसार खो दिया।” [२१७]
तांत्रिक परंपराओं में जो यौन अभ्यास के हिस्से के रूप में सेक्स का उपयोग करते हैं (यह मुख्य रूप से कौल और तिब्बती बौद्ध धर्म को संदर्भित करता है), सेक्स और इच्छा को अक्सर पारगमन के साधन के रूप में देखा जाता है जिसका उपयोग निरपेक्षता तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, सेक्स और इच्छा को अपने आप में अंत के रूप में नहीं देखा जाता है। चूंकि ये प्रथाएं धार्मिक पवित्रता के रूढ़िवादी हिंदू विचारों का उल्लंघन करती हैं, इसलिए उन्होंने अक्सर भारत में तंत्र को एक खराब छवि दी है, जहां अक्सर रूढ़िवादी इसकी निंदा करते हैं। पैडौक्स के अनुसार, इन प्रथाओं को स्वीकार करने वाली परंपराओं में भी, वे प्रमुख से बहुत दूर हैं और केवल “कुछ पहल और पूरी तरह से योग्य निपुण” द्वारा अभ्यास किया जाता है। [२१८]
पश्चिमी विद्वानों के अनुसंधान
श्री यंत्र (तीन आयामी रूप में जाना जाता प्रक्षेपण में यहाँ दिखाया गया है श्री मेरु या महा मेरु , द्वारा मुख्य रूप से इस्तेमाल श्रीविद्या शाक्त संप्रदायों)।
जॉन वुडरॉफ
तंत्र का गंभीरता से अध्ययन करने वाले पहले पश्चिमी विद्वान जॉन वुड्रोफ (1865-1936) थे, जिन्होंने तंत्र के बारे में आर्थर एवलॉन नाम से लिखा था और उन्हें “तांत्रिक अध्ययन के संस्थापक पिता” के रूप में जाना जाता है। [२१९] पिछले पश्चिमी विद्वानों के विपरीत, वुडरोफ ने तंत्र की वकालत की, वेदों और वेदांत के अनुसार इसे एक नैतिक और दार्शनिक प्रणाली के रूप में बचाव और प्रस्तुत किया । [२२०] वुडरॉफ ने तंत्र का अभ्यास किया और, शैक्षिक निष्पक्षता बनाए रखने की कोशिश करते हुए, हिंदू तंत्र ( शिव-शाक्त परंपरा) का छात्र था । [२२१] [२२२] [२२३]
इससे आगे का विकास
वुडरोफ के बाद, कई विद्वानों ने तांत्रिक शिक्षाओं की जांच शुरू कर दी, जिसमें तुलनात्मक धर्म और इंडोलॉजी के विद्वान जैसे कि अगेहानंद भारती , मिर्सिया एलियाडे , जूलियस इवोला , कार्ल जंग , एलेक्जेंड्रा डेविड-नील , ग्यूसेप टुकी और हेनरिक ज़िमर शामिल हैं । [२२४] ह्यूग अर्बन के अनुसार, ज़िमर, इवोला और एलियाडे ने तंत्र को “सभी भारतीय विचारों की परिणति: आध्यात्मिकता का सबसे कट्टरपंथी रूप और आदिवासी भारत का पुरातन हृदय” के रूप में देखा, इसे आधुनिक युग के लिए आदर्श धर्म के रूप में देखा। तीनों ने तंत्र को “पवित्र के लिए सबसे अधिक आक्रामक और हिंसक मार्ग” के रूप में देखा। [225]
यह सभी देखें
नियोतंत्र